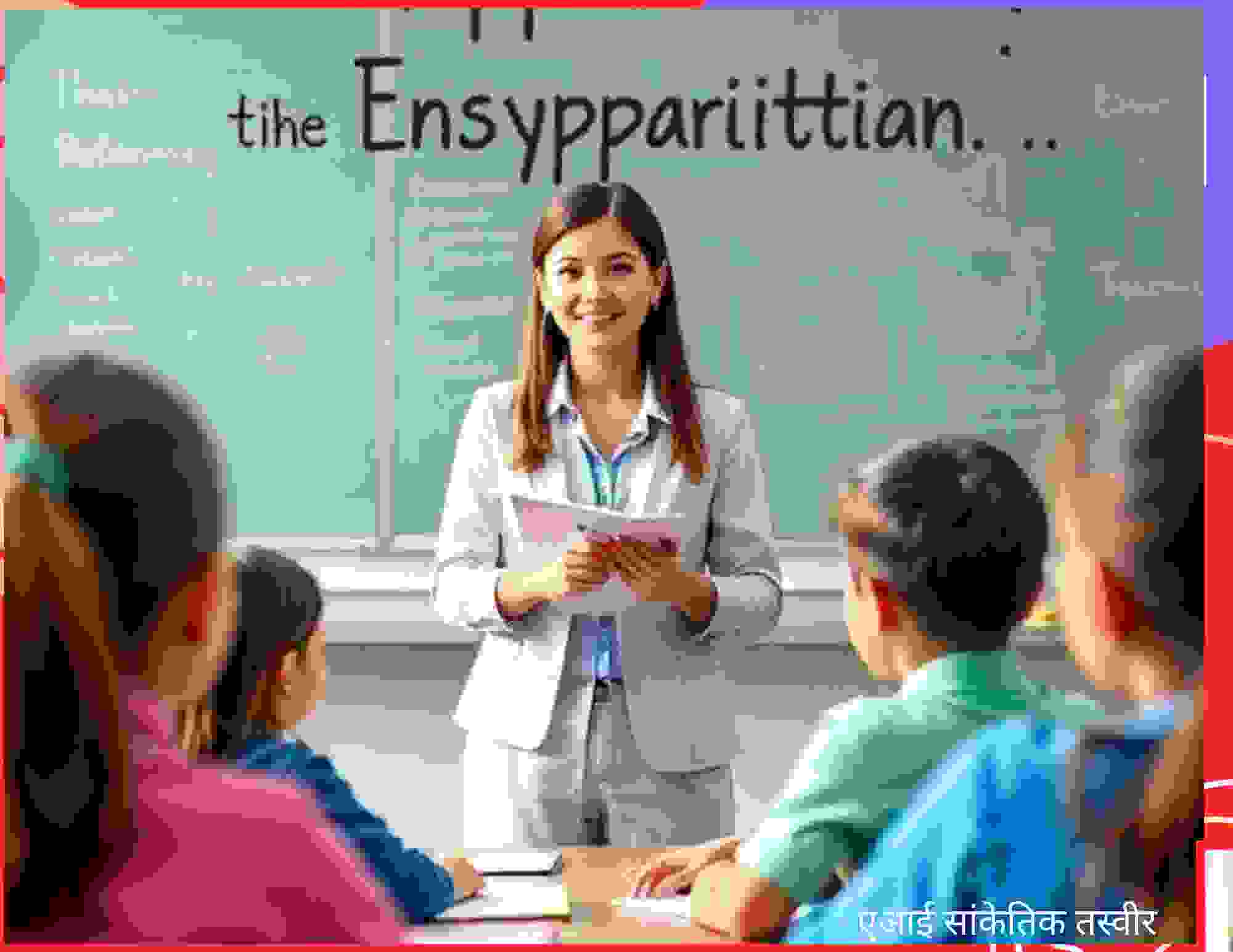अनिल अनूप
हर सुबह जब अखबार के पन्ने खुलते हैं या मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज़ अलर्ट चमकता है, तब सबसे ज़्यादा जो खबरें ध्यान खींचती हैं, वो होती हैं – “बच्ची के साथ दुष्कर्म”, “दिनदहाड़े हत्या”, “महिला की अस्मत लूटी”, “दो पक्षों में खूनी संघर्ष” जैसी सनसनीखेज हेडलाइंस। ये खबरें अब दुर्लभ नहीं रहीं, बल्कि आम होती जा रही हैं। एक पत्रकार और विशेषकर एक संपादक के लिए यह दौर सबसे कठिन हो गया है। वह रोज एक अजीब सी मनोदशा से गुजरता है, जहां उसकी आत्मा, उसका विवेक, उसकी पत्रकारिता की मूल भावना बार-बार सवाल उठाती है – “क्या ये ही पत्रकारिता है?”
खबरों की दौड़ में विवेक का संघर्ष
एक संपादक के लिए खबरों का चयन करना महज एक पेशेवर कार्य नहीं है, बल्कि यह उसकी सोच, उसकी चेतना और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रतिफल होता है। वह जानता है कि हत्या और बलात्कार की खबरें लोगों को चौंकाती हैं, उन्हें पढ़ने पर मजबूर करती हैं और ट्रैफिक बढ़ाती हैं। लेकिन वह यह भी जानता है कि इन खबरों के पीछे टूटे हुए परिवार, बर्बाद जिंदगियाँ, और सामाजिक असुरक्षा की भयावह कहानियाँ छुपी होती हैं।
आज का संपादक अपने विवेक और बाज़ार की मांग के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। वह जानता है कि अगर वह ये खबरें नहीं चलाएगा, तो कोई और चलाएगा। और जब बाकी मीडिया इन्हें दिखा रहा होगा, तो उसकी निष्क्रियता उसकी टीम, उसके पोर्टल, उसकी नौकरी, यहाँ तक कि उसकी पहचान को भी सवालों के घेरे में ला देगी।
जब अपराध “नॉर्मल” हो गया
समस्या यह नहीं है कि हत्या और रेप की घटनाएं हो रही हैं। दुर्भाग्यवश, ये हमेशा से रही हैं। समस्या यह है कि इनकी आवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये हमें चौंकाती नहीं, बल्कि हमारे लिए “नॉर्मल” हो गई हैं। यही “नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ क्राइम” एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। जब एक 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर को पढ़कर भी पाठक की आंखें नम नहीं होतीं, तब संपादक के भीतर कुछ मर जाता है।
वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वह समाज को हिंसा और अपराध का इतना आदि बना चुका है कि अब यह सब सामान्य लगने लगा है? क्या उसका काम खबरें देना है या खबरों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करना और समाज को दिखाना?
संपादक की पीड़ा: “चलाना ज़रूरी है, लेकिन…”
संपादक की पीड़ा यह है कि वह जानता है कि हत्या और बलात्कार की घटनाएं सनसनीखेज हेडलाइन बनाती हैं, ट्रेंड में रहती हैं, और पेजव्यू लाती हैं। वह यह भी जानता है कि जब तक ये खबरें वायरल नहीं होंगी, तब तक प्रशासन नहीं जगेगा, न्याय प्रणाली हरकत में नहीं आएगी और जनदबाव नहीं बनेगा।
लेकिन दूसरी ओर, वह यह भी महसूस करता है कि बार-बार इन खबरों को दिखाना कहीं न कहीं अपराधियों के मन से भय हटाता है। उन्हें लगता है कि ऐसी खबरें तो रोज़ आती हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई! समाज भी सोचने लगता है कि “चलो, हमारे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ होता रहता है।”
एक ईमानदार संपादक इस दुविधा में रोज़ जीता है। वह खबर को प्रकाशित करते समय एक पल के लिए ठहरता है, सोचता है – “क्या इसे थोड़ा अलग ढंग से दिखाया जाए? क्या हम इसमें अपराधी की बर्बरता से ज़्यादा पीड़िता की कहानी को सामने लाएं? क्या हम समाज से एकजुटता की अपील करें, सिर्फ सनसनी न फैलाएं?” लेकिन तब उसे तकनीकी टीम की मीटिंग याद आती है – “ट्रैफिक गिरा है सर, कुछ तेज हेडलाइंस चाहिए।”
पत्रकारिता की आत्मा बनाम टीआरपी की लड़ाई
आज की पत्रकारिता का एक क्रूर सत्य है – TRP sells, pain doesn’t. समाज की संवेदनाएं अब स्क्रॉल होती खबरों की गति पर टिकी हैं। तेज हेडलाइन, खून के छींटों से सनी फोटो और आक्रोश से भरे वीडियो क्लिप ही सोशल मीडिया पर ‘अंगेजमेंट’ लाते हैं। संपादक के पास सीमित समय होता है, सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन अपेक्षा यही होती है कि वह ‘बिग ब्रेकिंग’ दे।
और यह ‘बिग ब्रेकिंग’ अक्सर किसी की मौत, किसी की इज्जत की आहूति या किसी की बर्बादी से ही आती है।
क्या संपादक को यह खबरें पसंद हैं? नहीं। क्या वह उन्हें रोक सकता है? शायद नहीं। क्या वह उन्हें न चला कर अपना योगदान दे सकता है? शायद, लेकिन तब उसकी आवाज़ ही नहीं बचेगी।
समाज की चुप्पी और पत्रकार की बेबसी
इस पूरे परिदृश्य में एक और चीज़ बहुत खलती है – समाज की चुप्पी। अपराध की खबरें जितनी तेजी से फैलती हैं, उतनी ही जल्दी भुला दी जाती हैं। कोई ठहरकर यह नहीं सोचता कि इस अपराध का मूल कारण क्या था? क्या प्रशासन की विफलता थी, क्या सामाजिक मूल्यों का पतन था, क्या बेरोजगारी, शराबखोरी, या लचर कानून व्यवस्था जिम्मेदार थी?

जब समाज सवाल करना छोड़ देता है, तब पत्रकार की लड़ाई और कठिन हो जाती है। वह अकेला पड़ जाता है। उसकी खबरें सिर्फ ‘उपभोग’ की वस्तु बन जाती हैं, बदलाव का माध्यम नहीं।
फिर भी उम्मीद बची है…
संपादक टूटता है, मगर फिर भी हर सुबह अपनी डेस्क पर बैठता है। वह फिर से खबरों की छंटनी करता है। वह अब भी किसी कहानी में “उम्मीद की किरण” खोजने की कोशिश करता है – किसी सामाजिक आंदोलन, किसी निर्भीक लड़की, किसी साहसी पुलिस अफसर, या किसी आम नागरिक की कहानी को प्रमुखता देने की।
क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ चीखते हेडलाइन की कला नहीं है, यह समाज का दस्तावेज़ है। और यह दस्तावेज़ तब ही प्रामाणिक बनता है जब वह दुख के साथ-साथ आशा को भी दर्ज करे।
एक संपादक की आत्मा कभी नहीं चाहती कि वह रोज हत्या, बलात्कार, और हिंसा की खबरें चलाए। लेकिन वह जानता है कि जब तक ये घटनाएं घट रही हैं, जब तक न्याय अधूरा है, जब तक समाज चुप है – तब तक उसे बोलना होगा, दिखाना होगा, और लिखना होगा।
वह मजबूर है, मगर विवेकहीन नहीं। वह बेबस है, मगर निर्विकार नहीं। उसकी कलम अब भी भीतर के इंसान की पुकार सुनती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताक़त है – और यही पत्रकारिता की असली आत्मा भी।
अगर आप उससे उम्मीद रखेंगे, तो वह जरूर कोशिश करता रहेगा कि खबरें सिर्फ सूचना न रहें, चेतना बनें। यही संघर्ष, यही द्वंद्व उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और परीक्षा है।