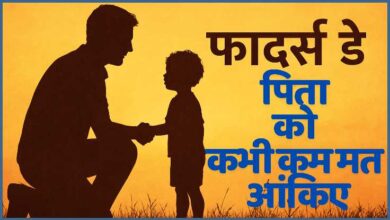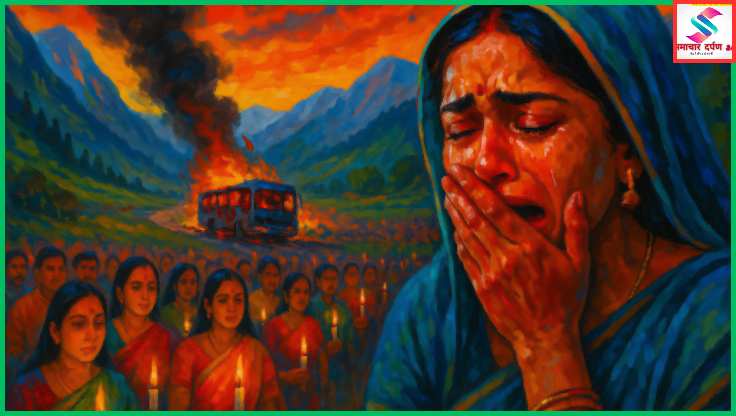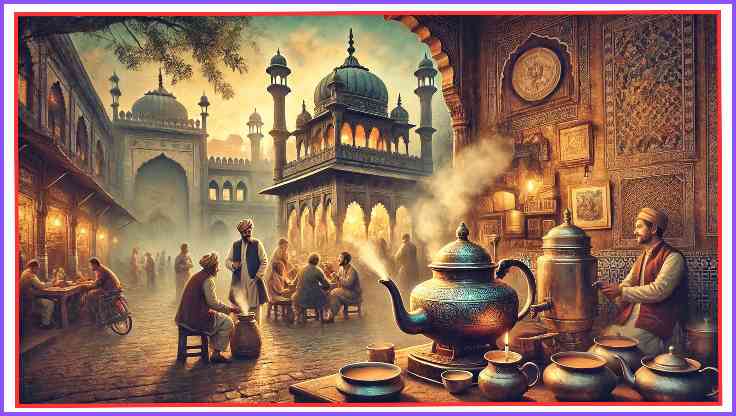इस आत्मकथात्मक लेख में एक वरिष्ठ लेखक की पीड़ा, विपन्नता और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बेरुख़ी का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह कथा न केवल व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है, बल्कि मानवीय गरिमा की रक्षा की पुकार भी करती है।
शब्दों के सौदागर की चुप चीख़: एक लेखक की आत्मकथा
शब्दों से जीवन रचने वाला मैं, एक वयोवृद्ध लेखक, आज स्वयं जीवन की संध्या में शब्दहीन सा पड़ा हूँ। वर्षों तक कलम से समाज को दिशा देने का प्रयास करता रहा; कभी उपेक्षित पीड़ाओं को स्वर दिया, तो कभी न्याय की चुप आवाज़ को गूंज में बदला। परंतु विडंबना देखिए, जब मेरे अपने जीवन में अंधकार घिर आया, तो इस तथाकथित ‘कल्याणकारी’ व्यवस्था ने मेरी आवाज़ तक को अनसुना कर दिया।
विगत कुछ वर्षों से मैं एक सीमित पेंशन और कभी-कभार मिलने वाली लेखकीय रॉयल्टी के सहारे जैसे-तैसे अपना जीवन जी रहा था। कभी साहित्य अकादमी से सम्मान मिला था, पर सम्मान भूख नहीं मिटाता, और न ही दवाइयों का विकल्प बन सकता है।
फिर एक दिन, अनचाहे ही बीमारी ने मुझे जकड़ लिया—काया कांपने लगी, हृदय ने शिकायत की और सांसों ने बोझिल होना शुरू कर दिया। घबराया नहीं, क्योंकि सोचा था कि देश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था अब विकसित हो चुकी है। पर वास्तविकता इससे कोसों दूर थी।
जब अस्पताल पहुँचा, तो उपचार से पहले मुझसे पूछा गया—”किसकी सिफारिश लाए हो?”
मैं स्तब्ध रह गया। वर्षों की सेवा, लेखनी के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन, क्या वह सब व्यर्थ था?
सहसा, मुझे एहसास हुआ कि इस व्यवस्था में जीवित रहने के लिए भी ‘पहचान’ आवश्यक है—वह पहचान जो रिश्वत, पैरवी या प्रभाव से मिलती है, न कि कर्म और समर्पण से। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि निजी अस्पताल की ओर रुख कर सकूँ, और सरकारी अस्पताल की लंबी पंक्तियाँ, कठोर प्रशासनिक प्रक्रिया, और अप्रभावी व्यवस्था ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया।
दवाइयों की सूची लम्बी थी और आय कम। अंततः एक पुराने विद्यार्थी ने किसी मंत्री तक मेरी बात पहुँचाई, और तभी जाकर इलाज का मार्ग प्रशस्त हुआ। पर इस उपकार का बोझ मुझ पर अब भी है, जो मेरे आत्मसम्मान पर हर दिन एक घाव की तरह रिसता रहता है।
दवाइयों की सूची लम्बी थी और आय सीमित। सरकारी अस्पताल में जिन जीवनरक्षक दवाओं की आवश्यकता थी, वे ‘स्टॉक में नहीं’ की मुहर के साथ मुझे बाहर की दुकानों की ओर धकेल चुकी थीं। मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हर दवा खरीद सकूँ, और स्वास्थ्य की बिगड़ती दशा के बीच मैं स्वयं को एक खोखले इंतज़ार में पाता रहा।
इसी समय, मेरे एक पुराने पाठक, जो एक शिक्षक हैं और समाज-सुधार की चेतना से संलग्न रहते हैं, का फोन आया। वह वर्षों से मेरे लेखन से प्रेरणा लेते रहे हैं और अवसर मिलते ही मुझसे संवाद करने की इच्छा रखते थे। जब उन्होंने मेरी अवस्था जानी, तो एक शब्द भी कहे बिना अपना सहारा दिया।
उस क्षण, मैं मौन था, पर भीतर कहीं एक संताप पिघलने लगा। उनकी आँखों में वह श्रद्धा थी, जो किसी लेखक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होती है। मैं जानता हूँ, यह एक साधारण सहायता नहीं थी, यह उस सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिध्वनि थी, जो कभी मेरे शब्दों से जन्मी थी और अब मेरे जीवन की संध्या में लौटकर आश्रय बन गई।
मैं उनके प्रति हृदय से साधुवाद करता हूँ। वे उस समाज के प्रतिनिधि हैं, जो संवेदना से संपन्न है और जहाँ मनुष्यता अब भी जीवित है। यदि इस देश में ऐसे शिक्षक और नागरिक बढ़ें, तो न केवल लेखक, बल्कि हर उपेक्षित आत्मा को संबल मिल सकेगा।
अब सोचता हूँ, क्या मेरे जैसे हजारों लेखक, कवि, कलाकार जो निःस्वार्थ भाव से देश की सांस्कृतिक नींव को मजबूत करते रहे, क्या उनका इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं? क्या सम्मान केवल पुरस्कार समारोहों तक सीमित रह गया है?
अंत में, मैं यही कहना चाहूँगा—यह आत्मकथा मेरी नहीं, हर उस संवेदनशील आत्मा की है जो व्यवस्था की दया पर नहीं, अधिकार पर जीना चाहती है।
अगर शब्द सचमुच सशक्त होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पंक्तियाँ व्यवस्था के हृदय को झकझोरें, और एक नई संवेदना का संचार करें।
➡️अनिल अनूप