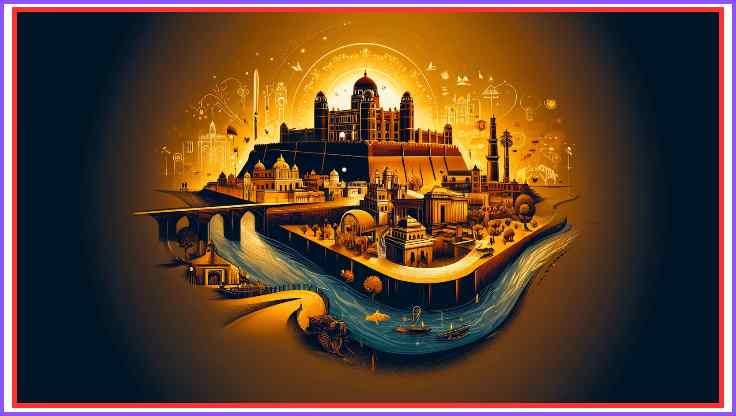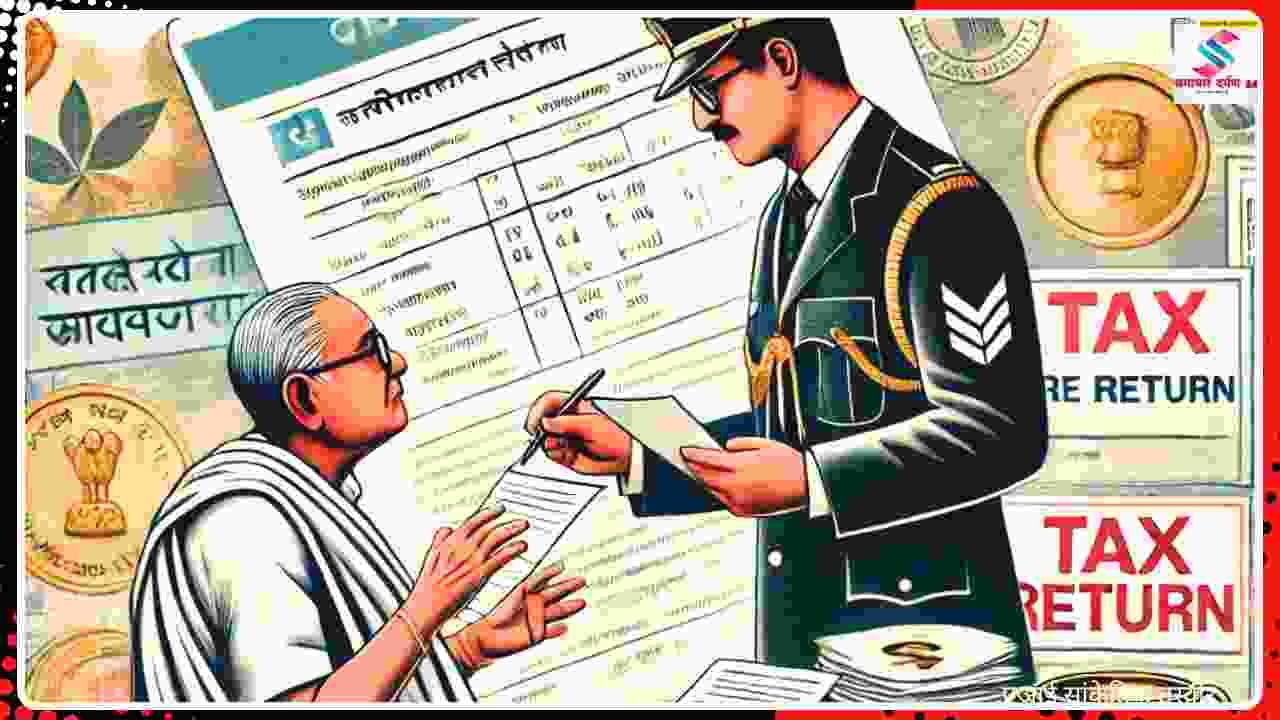अनिल अनूप
धरती के बाद अब समुद्र के भीतर छिपे खनिजों पर उद्योगों की नजर पड़ चुकी है. खनिज, जो बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनकी लगातार कमी होती जा रही है. इस कमी के अन्तर को पाटने के लिए समुद्र के दोहन की कोशिशे तेज हो गई है. यह सोच वैसे तो 1982 में बन चुकी थी कि समुद्र में अथाह सम्पदा है और इसका भी दोहन विकास के लिए होना चाहिए. इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी’ बना दी गई. इसके उद्देश्य खनिज सम्पदा के दोहन के सन्दर्भ में देशों पर नियंत्रण रखना और उन्हें अनुमति प्रदान करना है.
सीमेंट और कंकरीट के निर्माण कार्यों में रेत का उपयोग अपरिहार्य है. आबादी बढ़ने के साथ-साथ आवास, स्कूल, अस्पताल, सड़क हों या पेयजल भंडारण से जुड़ी जरूरतें सभी कि निर्माण में रेत, सीमेंट, कंकरीट आदि की मांग तेजी से बढ़ी है. रेत में भी प्राथमिकता में मांग नदियों से निकलने वाली रेत की है. इसलिए भारत सहित दुनिया भर में ही नदियों से रेत खनन अत्यधिक होने लगा है. गैर-कानूनी रेत खनन का कारोबार पूरे देश में ही आपराधिक हिंसक प्रवृत्तियों के साथ जड़ें जमा चुका है.
गुजरात में साबरमती नदी में रेत का इतना अवैध खनन होता रहा है कि अहमदाबाद, साबरकांठा, गांधीनगर जिलों में इन पर निगाह रखने के लिए 2018 में ड्रोन से निगरानी तक की गई. यह स्थिति तब है जब 2016 के बाद साबरमती नदी में गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच रेत खनन पूरी तरह से रोक दिया गया था और इस बीच के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया गया था. गुजरात सरकार ने स्वीकार किया था कि राज्य में अवैध खनन बहुत गंभीर समस्या है. अन्य राज्य भी इस समस्या से बचे नहीं हैै. राज्य विधानसभाओं में भी इस पर चर्चा होती है, लेकिन अवैध रेत खनन नहीं हो रहा है, ऐसा न सत्तारूढ़ दल कहता है न विपक्ष.
रेत खनन से नदियों की पारिस्थितिकीय प्रणालियों के साथ-साथ तटीय क्षरण, नदी तलहटियों की भू-आकृतीय संरचनाओं में बदलाव मछलियों, घड़ियालों, कछुओं जैसे जलजीवों के आवागमन व प्रजनन क्षेत्रों में अवरोध और आत्मरक्षा के लिए उनके छुपने के क्षेत्रों पर संकट भी आ जाता है. गंगा की ही बात लें तो वैज्ञानिकों ने ही यह पुष्ट किया है कि रेत खनन से ऐसे कछुए, जिन्हें एक बार सफाई के लिए गंगा में डाला गया था अब लगभग समाप्त हो गए हैं. ये कचरे को नष्ट करने में मददगार होते थे। नदियों की वनस्पतियां भी रेत से खनन प्रभावित होती हैं. रेत कई तरह के प्रदूषण से बचाने में मददगार होती है. इससे पानी की गुणवत्ता ठीक रखने में भी मदद मिलती है.
नदी तलहटियों से रेत खनन से नदियों में जल प्रवाह की दशा व गति पर भी असर पड़ता है. आसपास की खेती भी इससे प्रभावित होती है. नदियों व पर्यावरण के लिए रेत के महत्व को स्वीकारते हुए अदालतों व सरकारी मानकों ने भी पर्यावरण हित में रेत खनन को नियमित व कई जगहों पर प्रतिबंधित किया है. निर्देशों में साफ कहा गया है कि पुलों और आवासीय बस्तियों के पास रेत खनन न हो. किंतु खनन वहां भी होता है. हद तो यह है कि घोषित ईको सेंसटिव व वन क्षेत्रों में भी अवैध खनन हो रहा है. कुल मिलाकर तथ्य यह है कि बिना प्रशासन की मदद के अवैध खनन नहीं हो सकता है.
इस बीच नदियों में रेत खनन के मामले को समग्रता में समझने का एक अवसर एनजीटी का एक हालिया निर्देश देता है. अप्रैल, 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार पर अवैध रेत खनन रोकने में असमर्थ रहने पर कुछ निर्देशों के साथ सौ करोड़ रुपए का अंतरिम दंड भी लगाया गया था. राज्य के मुख्य सचिव को अनियमित रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने के आदेशों के साथ-साथ यह भी चेताया गया था कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी है व उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी है. निस्संदेह एनजीटी यह भी जानता है कि रेत खनन का अवैध करोबार पूरे देश में आपराधिक तत्वों और माफियाओं के कब्जे में है और उसके पहले के निर्देश भी विभिन्न राज्यों में दिखावे के लिए स्वीकारें जाते हैं.
रेत की मांग के मुकाबले आपूर्ति में भारी कमी बनी हुई है. भारत में ही मांग को पूरा करने के लिए कुछ हद तक अवैध रेत खनन को कम करने के लिए कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे राज्य लाखों टन रेत आयात कर उपभोक्ता व उद्योगों को दे भी रहे हैं. निजी आयातकों के लिए यह लाभ का सौदा भी हो रहा है. 2017 से मलेशिया से ऐसा आयात जोर पकड़ रहा है. राज्य अपने यहां नदियों की रेत दूसरे राज्यों से मंगा कर बेच रहे हैं. इसके अलावा रेत की कमी पूरी करने के लिए स्टोन क्रैशरों से राज्यों के भीतर भी पत्थरों-चट्टानों से रेत निर्माण की मंजूरी दी जा रही है.
नतीजतन, कई जगहों पर लगभग पूरी पहाड़ियों को मटियामेट कर दिया है. अवैध रेत खनन की संभावनाएं तब भी बढ़ जाती हैं जब स्टोन क्रैशर भी नदियों के पास लगे हों. कई जगहों पर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने इनसे होने वाले वायु प्रदूषण, जल भंडारों व पारिस्थितिकीय नुकसानों पर विरोध भी जताया है. यह भी कहा जा सकता है जब पूरे समुद्रों में रेत हैं, रेगिस्तानों में रेत है तो फिर भारत में रेत के मशीनी उत्पादन की आवश्यकता क्यों हो जाती है? समुद्र की रेत लवणीय होने के कारण और रेगिस्तान की रेत गोल होने व कम खुरदुरी होने के कारण निर्माण के लिए आदर्श नहीं मानी जाती है.
यदि रेत खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में पहले से ही यह अध्ययन न किया गया हो कि वहां से कितनी रेत बंजरी पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए बिना निकाली जा सकती है तो वैध खनन से भी पर्यावरणीय हानि हो सकती है. वैज्ञानिक अध्ययनों और आंकड़ों की कमी के कारण रेत खनन से हुए कुप्रभावों का सही पता नहीं चल पाता है. जैसा कि आदेश में कहा गया है कि यदि खनन से कोई हानि हुई है तो उसकी भरपाई की जाए. निस्संदेह खनन के बाद वाले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी जरूरी हो गए हैं, क्योंकि तभी तो आप भरपाई की बात सोच सकते हैं.
नदियों में खनन का तो अब तक का यही इतिहास रहा है कि जितने खनन की अनुमति ली जाती है, उससे कई गुना ज्यादा का खनन होता है. बाद के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से ही पता चल पाएगा कि जितने खनिज, उपखनिज को निकाला जाना है व जिस जगह से निकाला जाना है. जिन तरीकों से और जिन मशीनों से निकाला जाना है, उनसे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में किनारों के भूजल भंडारण पर होने वाला अंतर, किनारों का कटाव, नए भूस्खलन, भू-धंसाव, भूक्षरण के संभावित क्षेत्रों का भी उल्लेख होता है.
दरअसल, विरोध रेत के अवैध खनन को लेकर है। लेकिन जिन पहलुओं को एनजीटी ने छुआ है वे वैध खनन पर भी समान रूप से लागू होते हैं. पर्यावरण प्रभाव और ट्रस्टीशिप संबंधी चिंता वैध और अवैध दोनों मामलों में प्रासंगिक है. वैध खनन पर तो निगरानी रखनी और भी आवश्यक है, क्योंकि भारी मात्रा में अवैध खनन, कानून की ही आड़ में होता है। स्वीकृत गहराइयों से दुगनी-तिगुनी गहराइयों तक पहुंच कर रेत खनन किया जाता है. जिन चिन्हित क्षेत्रों के एि रेत खनन पट्टा होता है उनसे बाहर जाकर भी खनन होता है.
ढुलाई वाहन पारपत्र पर दर्शाए गए माल से दुगना-तिगुना माल लेकर बेरोकटोक बाहर निकाले जाते हैं. ज्यादातर जगहों पर तो इन ढुलाई वाहनों पर नंबर प्लेट भी नहीं होती. पूरे देश में अवैध रेत खनन का कारोबार माफिया और आपराधिक तत्वों के हाथ में है. जो ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी रेत माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हैं उन पर रेत से भरे ट्रक, ट्रैक्टर चढ़ा देना, हत्या कर देना, उनका तबादला करवा देना माफिया के लिए आम है. माफिया में ऐसी हिम्मत उनके राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों व अपराधी तत्वों के साथ जगजाहिर संबंधों से आती है. इसलिए अवैध रेत खनन पर शिकंजा कस पाना संभव नहीं लग रहा.
दुनिया में कम्प्यूटर व स्मार्ट फोन का व्यापार तेजी से पनप रहा है. इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खनिज समुद्र में बहुतायात में उपलब्ध है. खासतौर से कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, जिंक, मैंगनीज आदि खनिज लगातार भू-खनन से समाप्ति की ओर हैं. इसीलिए अब विभिन्न देशों की दृष्टि समुद्र की ओर है. केवल स्मार्ट फोन और कम्प्यूटर तक ही इन खनिजों के उपयोग सीमित नहीं हैं, बल्कि मिल टरबाइन, सोलर पैनल व बैटरी आदि इन खनिजों पर निर्भर हैं. समुद्र खनन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 15 लाख वर्ग किमी के कॉन्ट्रेक्ट दिए जा चुके हैं.
समुद्र एक बड़ा पारिस्थिति तंत्र है और इसको एक नए उद्योग के रूप में देखे जाने तक बात खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए, जितने क्षेत्र में खनन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, उनमें प्रशांत, अटलांटिक व हिन्द महासागर खनन के लिए पहले दर्जे के स्थान होंगे. यद्यपि यह साफ नही है कि खनन किस तरह होगा, इसका क्या स्वरूप होगा, लेकिन यह तय है कि ये समुद्र में एक नई खलबली मचा देंगे. खासतौर से जब पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ चुका हो और अब समुद्र की बारी हो तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हालात क्या होंगे ? भारत भी पीछे नही है. यहाँ भी ‘डीप ओशन मिशन’ के तहत प्रोजेक्ट की पहल की है. इसमें पॉलीमेटेलिक खनिज जैसे-कोबाल्ट, मैगनीज, निकल का खनन होगा. करीब 6000 मीटर तलहटी में यह दोहन किया जाएगा. वैसे भारत को 1987 में ही खनन की अनुमति मिल गई थी.
ऐसा नहीं है कि समुद्र में होने वाले खनन के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की आशंकाएँ ही ना हों. ब्रिटेन के एक बड़े अखबार गार्जियन ने इसका विरोध करने के लिए कमर कसी है. लेकिन सीबेड अथॉरिटी ने दावा किया है कि जो भी खनन होगा, वो उचित तकनीक से होगा. पर सच तो यह है कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा अध्ययन व रिपोर्ट नहीं है, जो यह बता सके कि समुद्र में खनन की शैली क्या होगी ? इसमें प्रयोग होने वाले जो तमाम उपकरण होंगे, वे किस स्तर के होंगे. ऐसा कोई भी आधारभूत अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है. यही नही, इनके पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन की कोई जानकारी भी हमारे पास नही है. खनन क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहाँ विशिष्ट जीव प्रजातियाँ हैं और उनके पास सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती. फिर कुछ धातु जैसे- कोबाल्ट, मैगनीज, निकल आदि के विषैले प्रभाव भी होते हैं. यदि हमने समुद्र की तलहटी में खनन के लिए छेड़छाड़ की तो इसकी आशंका है कि यही तत्व पानी में भी घुलकर जहरीली परिस्थितियाँ पैदा करेंगे। फिर वहाँ की जीव प्रजातियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा. आज हम हर पारिस्थितिकी तंत्र को संकट में डाल रहे हैं, चाहे वह पृथ्वी का हो या समुद्र का. इस तरह के विकास, जिससे विनाश की आशंका रहती हो, इसके कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं. इसलिए ऐसी शुरुआत से पहले हमें एक गहरी समझ बनानी होगी. सबसे बड़ी बात इस कार्य से जनता को भी जोड़ना होगा और उसके माध्यम से एक आम सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे विकास में लाभ मुट्ठी भर लोगों का होता है, पर नुकसान सबको उठाना पड़ता है.
सूखी सूखी केन नदी
ऐतिहासिक भूरागढ़ किला दूर से ही दिखने लगता है और नीचे बहती केन नदी, पुल से दिखाई पड़ती है. वामदेवेश्वर पर्वत और पहाड़ के दोनों तरफ घनी बस्ती यह थी, बांदा की पहली पहचान. केन पुल के नीचे खूब भरी-भरी, चैड़ी केन नदी, जो कभी कर्णावती थी, जो रेल के पुल, फिर पुल के पार श्मशान और आगे वाले मोड़ तक मुश्किल से डेढ़ किलोमीटर का फासला, लेकिन इतने में ही केन की कितनी मुद्राएं. धोबी घाट, घुटरून पानी तेजी से दौड़ता, नीचे-नीचे दौड़ते रेत के कण, हम खुली आंखो में छींटे मारने का खेल खेला करते थे. इतना साफ पानी किसी नदी में देखने को नहीं मिला. आज उसी केन नदी पर खाकी का पहरा है. दूर से दूरबीन के सहारे उसी कल-कल बहते पानी की रखवाली हो रही है जहां पहले हम स्वछन्द खेलते कूदते थे.
दुनिया में ज्यादातर नदियां अपने तटवर्ती इलाकों के लिए जीवनदायिनी रही हैं. सभ्यताओं के विकास में नदियों का भोग बन रहा है. यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में आज नदियों का अस्तित्व खतरे में है. मध्यप्रदेश से निकलकर बुन्देलखंड क्षेत्र में खजुराहों और बांदा से होकर चिल्ला तक बहने वाली केन नदी आज संकट में है.
खनिज विभाग और बालू माफिया मिलकर नदियों का लाल सोना (बालू) लूट रहे हैं. भारी-भरकम पोकलैंड मशीनें नदी का सीना चीरकर बालू निकाल रही हैं, जिससे एक-एक ट्रक में एक-एक टैंकर पानी जा रहा है. मिट्टी तक बालू खनन करने से पानी का ठहराव कम होता जा रहा है, जिससे जलस्तर नीचे जा रहा है और केन नदी सूख रही है. हालत यह है कि जो केन नदी पूरे शहर को बिना किसी दिक्कत के पानी पिला रही थी आज उसी के पानी में जीवन पाने वाली मछलियों, अन्य जीव-जन्तुओं का जीवन खतरे में है. केन के तट में बसे आधा सैंकड़ा गांव ऐसे हैं जिनके जीने का सहारा बन गई थी केन, लेकिन आज सब कुछ बदल सा गया है. दिन-रात बालू खनन से बुन्देलखंड के जनपद बांदा की जीवन रेखा बन चुकी केन की धारा सूख रही है. कई स्थानों पर केन का पानी रोक लेने से यहां जलापूर्ति पर खासा असर पड़ा है. पानी न मिलने से लोगों को शासन प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा है. प्रशासन को जो कदम पहले उठाने चाहिए थे, वे उठाये नहीं. अब जब आन्दोलन होने लगे तो पानी की पहरेदारी शुरू हो गई.
राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया था कि अरावली की 138 में से 28 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं. इतना ही नहीं खनिज विभाग की ओर से साल भर कार्रवाई की गई, लेकिन जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई. वहीं एफएसआई सर्वे में सैटेलाइट से देखा तो अलवर जिले में 274 स्थानों पर अवैध खनन दिखा.अलवर जिला लंबे समय से अवैध खनन की समस्या से जूझ रहा है. पूर्व में तिजारा, भिवाड़ी क्षेत्र में खान माफिया ने इस कदर अवैध खनन किया कि कई पहाड़ ही खत्म हो गए, या फिर अरावली पर्वतमाला का स्वरूप ही बदल गया. अवैध खनन की बढ़ती समस्या के चलते कार्रवाई भी की गई, लेकिन अवैध खनन पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई. खनिज विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 में करीब 65 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, वहीं बीते साल विभाग की ओर से 45 करोड़ का राजस्व जुटाया गया. यानि खनिज विभाग ने सरकार का खजाना भरने में बीते साल से इस साल भूमिका निभाई.
आंकड़ों के अनुसार खनिज विभाग ने वर्ष 2017-18 में अवैध खनन के विरुद्ध 48 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली, वहीं वर्ष 2018-19 में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में वसूली 95 लाख रुपए तक पहुंच गई. यानि इस साल ज्यादा पेनल्टी वसूली गई. पेनल्टी वसूली में वृद्धि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल अवैध खनन हुआ, जिसकी सामग्री पत्थर व बजरी आदि अवैध तरीके से बिकने बाजार में आई और कार्रवाई के दौरान पकड़ी जाने पर उनसे पेनल्टी वसूल की गई.
अवैध खनन पर्यावरण के लिए ही नहीं लोगो की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है अवैध खनन देश कि प्रमुख समस्यां है जिसे रोकने पर कुछ हद तक प्रदूषण स्तर को रोका जा सकता है .