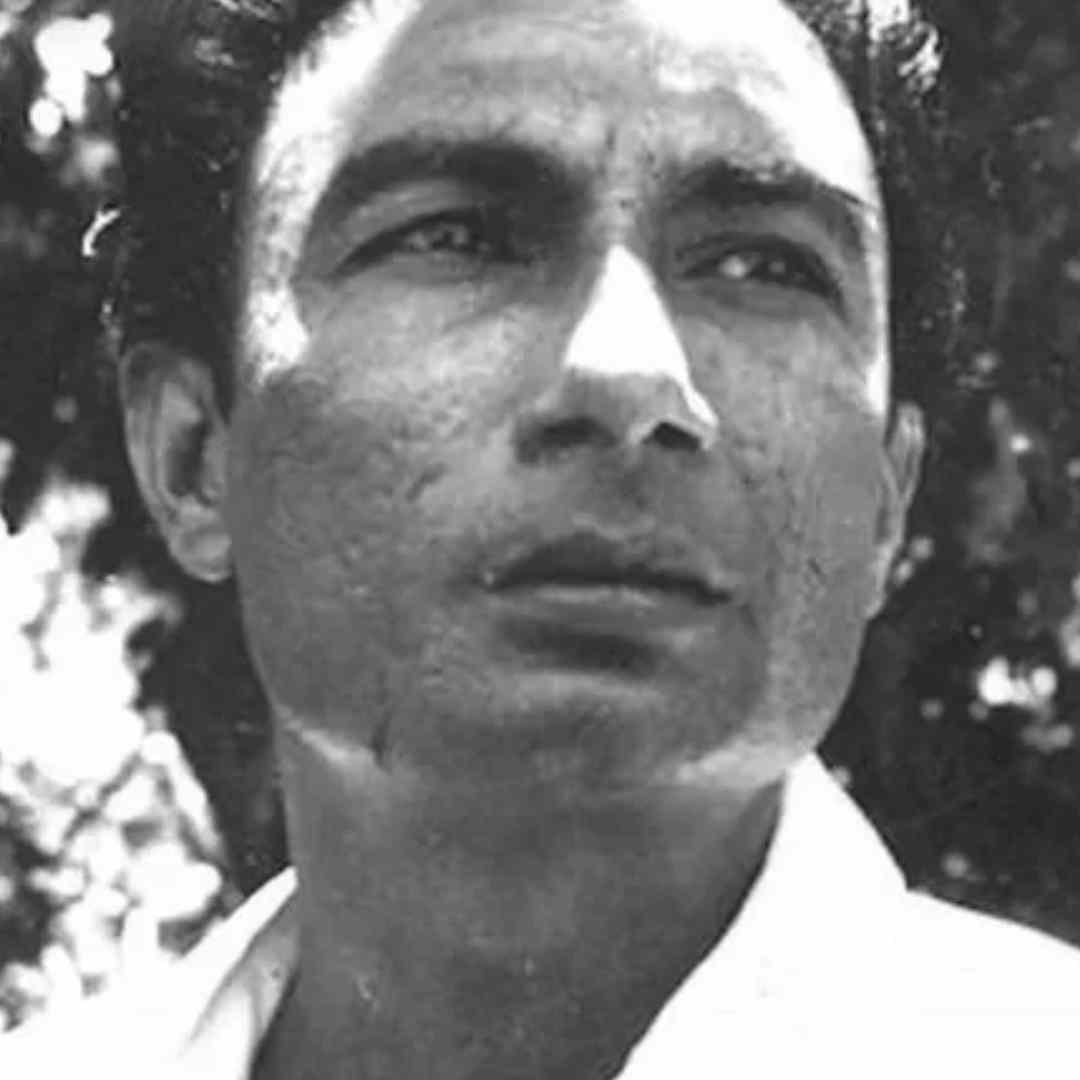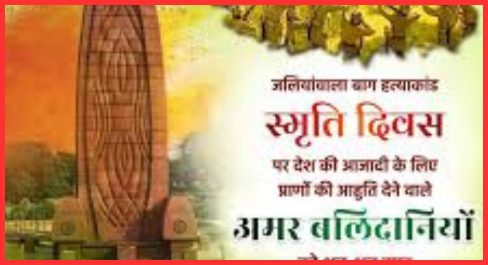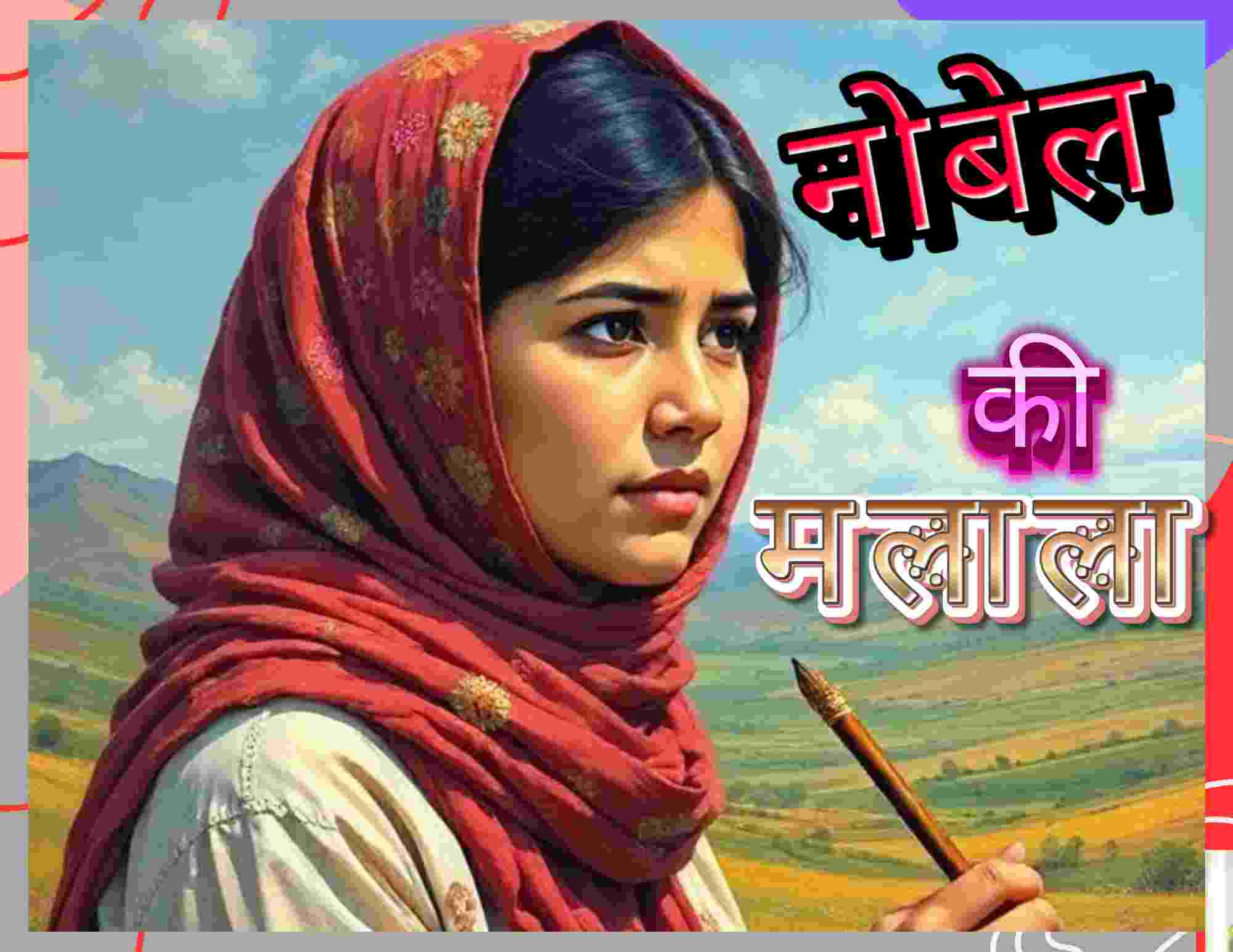अकील अब्बास जाफरी
साहिर लुधियानवी उन प्रमुख लेखकों और शायरों में से एक थे, जो 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे।
हमीद अख़्तर ने अपनी किताब ‘आशनाइयां क्या क्या’ में साहिर लुधियानवी के बारे में लिखा है कि “पाकिस्तान की स्थापना के बाद, मैं शरणार्थी कैंप के ज़रिए और साहिर हवाई जहाज़ से लाहौर पहुँचे। वह जून 1948 तक लाहौर में रहे। हमने एबट रोड पर एक मकान अलॉट कराया और साहिर, अम्मी और मैं एक साथ रहने लगे।
वो आगे लिखते हैं, “मैं लगभग तीन महीने तक कैंप में रहा। मैं नवंबर में लाहौर पहुँचा और साहिर सितंबर 1947 में पहुँचे थे। साहिर इस पूरे समय में उखड़े-उखड़े से रहे। मेरे आने से उन्हें कुछ हिम्मत तो मिली, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक असुरक्षित लग रहे थे।
‘सवेरा’ के संपादन से महीने के 40-50 रुपये मिल जाते थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थे और इस आमदनी में कुछ इज़ाफ़ा होने के भी कोई आसार नहीं दिख रहे थे।
हमीद अख़्तर लिखते हैं कि जून 1948 में उन्हें किसी काम से एक हफ़्ते के लिए कराची जाना पड़ा और उस एक महीने में कोई पत्राचार भी नहीं हो सका।
उन दिनों टेलीफ़ोन आम नहीं थे। फिर किसी ने उन्हें (साहिर को) बताया कि मुझे कराची में गिरफ़्तार कर सिंध पुलिस ने किसी जेल में डाल दिया है और अब वहां से मेरे बच निकलने की उम्मीद बहुत कम है।
ख़ुफ़िया पुलिस वाले साहिर को बहुत ख़तरनाक आदमी मानते थे। इसलिए उन्होंने उसे यहाँ से भगाने के लिए एक राजनीतिक मुख़बिर की मदद ली। वह रोज़ाना आकर साहिर को डराता था और कहता कि पुलिस उसे गिरफ़्तार करके शाही क़िले में ले जाएगी। वहां बड़े-बड़े सांप और बिच्छू होते हैं, यातना देने के अजीब तरीक़े होते हैं, वग़ैरह।
हमीद अख़्तर लिखते हैं, “यह चाल काम कर गई थी। अगर मैं वहां होता तो शायद उन्हें कुछ हौसला होता, लेकिन यारों ने मुझे तो पहले ही पुलिस के हवाले कर दिया था। साहिर इतना डर गया था कि एक दिन उसने अचानक दिल्ली आने का फ़ैसला कर लिया। उन दिनों, पासपोर्ट और वीज़ा वग़ैरह की कोई ज़रुरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने फ़र्ज़ी नाम से टिकट ख़रीदा और विमान में सवार हो गए।”
“अपने हिसाब से उन्होंने ये यात्रा ख़ुफ़िया तौर पर की। जून की गर्म दोपहर में, वह एक लंबा कोट और हैट पहनकर एयरपोर्ट पर पहुँचे। कहा जाता है कि जिन लोगों से छुप कर वह एयरपोर्ट गए थे, वो लोग एयरपोर्ट तक उनके पीछे-पीछे गए और वापस आकर रिपोर्ट लिखी। ‘साहिर लुधियानवी देश छोड़ कर चला गया है’।”
साहिर को पुलिस से डराने वाला दोस्त कौन था?
अहमद राही ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने इस घटना के काफ़ी समय बाद, 1995 में जब साहिर की कविताओं का संकलन ‘कुल्लियात-ए-साहिर’ प्रकाशित हुआ तो उसके प्रस्तावना में लिखा कि, “साहिर के अंदर सीआईडी का डर, आग़ा शोरिश काश्मीरी ने पैदा किया था। शोरिश साहिर के सच्चे हमदर्द और और शुभचिंतक थे। वह तो हमदर्दी के तौर पर साहिर को आने वाली परेशानियों के बारे में ख़बरदार कर रहे थे, लेकिन साहिर भीतर से हिल गए थे।”
अहमद राही आगे लिखते हैं, “साहिर अपनी नज़्मों में जितने निडर दिखते हैं, अपने व्यावहारिक जीवन में वो उतने ही डरपोक थे। उन्हें हर समय एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत रहती थी, शुरुआत से ही उन्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत रही। लुधियाना में चौधरी फ़ैज़ुल हसन, अनवर मुर्तज़ा, इब्ने इंशा और हमीद अख़्तर वग़ैरह उनके साथ होते थे। साहिर जब अमृतसर के एमएओ कॉलेज में मुशायरा पढ़ने आए, तो उनके साथ उनके एक मित्र जय देव भी आये थे, जिन्हें उन्होंने संगीत निर्देशक बना दिया था।”
वह आगे लिखते हैं कि “बॉम्बे जाते समय वह (साहिर) हमीद अख़्तर को अपने साथ लेकर गए थे और उन्हें भी अपनी फ़िल्म कंपनी में काम दिलाया था। जब पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आए तो मैं और चौधरी नज़ीर उनके साथ होते थे। भारत लौटने के बाद, प्रकाश पंडित उनके रक्षक बने रहे। हो सकता है कि साहिर का शोरिश से संबंध इसी कारण हो, क्योंकि शोरिश बहुत दबंग और बहादुर थे।”

साहिर लुधियानवी अपनी आत्मकथा ‘मैं साहिर हूँ’ में लिखते हैं, “मुझे ख़बर मिली कि हमीद को कराची में गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब मैं ख़ुद को असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन, जून 1948 की चिलचिलाती गर्मी में, शर्लक होम्स (मफ़लर, ओवरकोट, काले चश्मे और एक अंग्रेज़ी टोपी पहने हुए) के वेश में, मैं भारत आने के लिए निकल पड़ा।”
”सूरज इतना गर्म था कि चील तक ने अंडे छोड़ दिए थे। चोटी से एड़ी तक पसीना बह रहा था, मैं गर्मी की वजह से साँस नहीं ले पा रहा था। ज़ाहिर सी बात है इतनी गर्मी में ओवरकोट में लिपटा, एक छोटा सा सूटकेस लिए तांगे पर बैठा, मैं स्पष्ट रूप से दूसरों को बहुत अजीब लग रहा था। मैं इतना सहमा और घबराया हुआ था कि मैं डर के मारे बार-बार इधर-उधर देख रहा था। ज़ाहिरी तौर पर, मैं अपनी तरफ़ से शांत और लापरवाह रहने की बहुत कोशिश कर रहा था।”
साहिर लिखते हैं, “ये मेरी ख़ुशक़िस्मती थी कि उन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिए वीज़ा और पास पोर्ट की ज़रुरत नहीं थी। इसलिए मैं बहुत ही ख़ामोशी से लाहौर के वाल्टन हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। एक महीने बाद जब हमीद अख़्तर लाहौर वापस लौटे, तो घर ख़ाली देखकर हैरान रह गए। मैं और मेरी मां वहां नहीं थे, जो उनके अनुसार मकान को घर का दर्जा दे चुके थे और सभी दोस्तों की मेहमान नवाज़ी करते थे।”
साहिर दिल्ली पहुँचे
जब साहिर दिल्ली पहुँचे तो उन्हें प्रगतिशील साहित्यिक पत्रिका ‘शाहराह’ के संपादन का काम सौंप दिया गया। प्रकाश पंडित ने इस पत्रिका में उनके सहायक संपादक के रूप में काम किया। यहां उन्होंने इस पत्रिका के दो अंक प्रकाशित किए। इसी दौरान उन्होंने सरदार ग़ौर बख़्श की पत्रिका ‘प्रीत लड़ी’ का भी संपादन किया।
दिल्ली में उनकी मुलाक़ात जोश मलीहाबादी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, अर्श मुलसियानी, बलवंत सिंह, बिस्मल सईदी, जगन्नाथ आज़ाद और कश्मीरी लाल ज़ाकिर से हुई, लेकिन कुछ ही महीने बाद मई 1949 में वे बॉम्बे चले गए, जहां एक उज्जवल भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा था।
फ़िल्मी सफ़र
बॉम्बे में साहिर ने बहुत ही संघर्ष के बाद फ़िल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और भारत के सबसे लोकप्रिय फ़िल्मी शायर बन गए। उन्होंने बहुत सी फ़िल्मों को अपने गीतों से सजाया जिनमें ‘आज़ादी की राह पर’, ‘नौजवान’, ‘बाज़ी’, ‘प्यासा’, ‘मिलाप’, ‘साधना’, ‘जाल’, ‘अंगारे’, ‘अलिफ़ लैला’, ‘शहंशाह’, ‘धूल का फूल’, ‘ताजमहल’, ‘फिर सुबह होगी’, ‘अंदाज़’, ‘दाग़’, ‘कभी-कभी’ और ‘इन्साफ़ का तराज़ू’ जैसी फ़िल्में शामिल थीं।
उन्होंने फ़िल्म ‘ताजमहल’ और ‘कभी-कभी’ के लिए फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार हासिल किया।
साहिर लुधियानवी के कई शायरी संग्रह प्रकाशित हुए जिनमें ‘तल्ख़ियां’, ‘परछाइयां’, ‘गाता जाए बंजारा’ और ‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें’ शामिल हैं।
साल 1970 में, उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। साल 1972 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2013 में भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम से एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था।
25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। उनका असली नाम अब्दुल हई था।