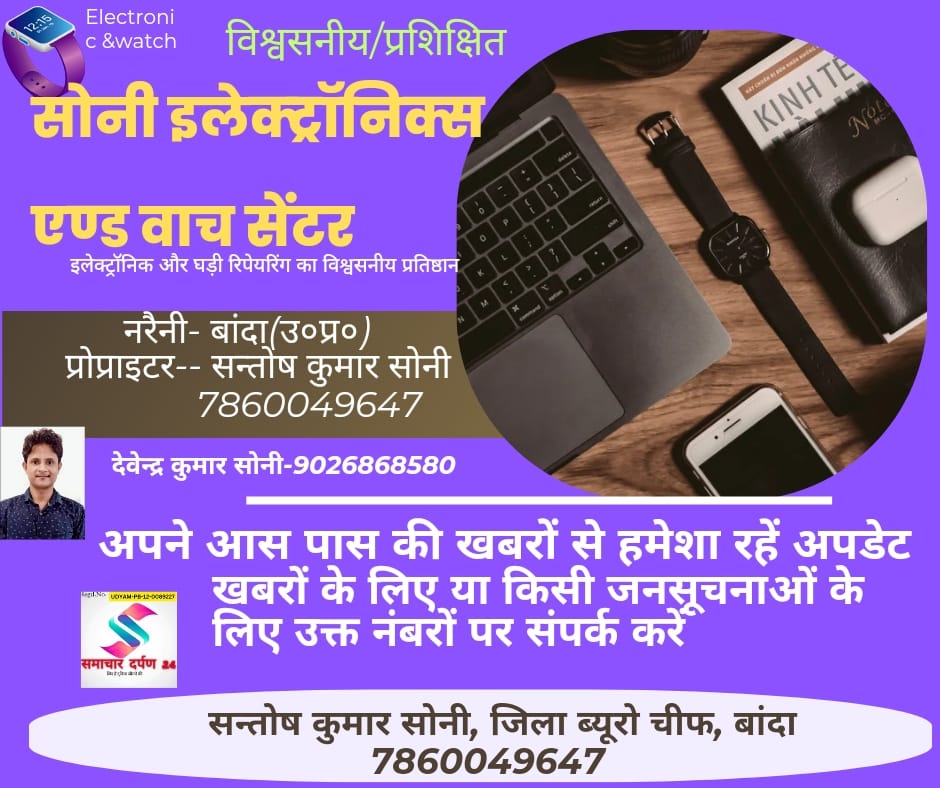अनिल अनूप
इस व्यंग्य में उन लोगों की पोल खोली गई है जो अपने स्वार्थ के लिए रंग बदलते रहते हैं। जो कल तक नफरत की आग भड़का रहे थे, वही आज शांति के मसीहा बनकर मंच पर खड़े हैं। जिन हाथों ने बस्तियों को जलाया, वही आज घायलों पर मरहम लगाने का ढोंग कर रहे हैं। राजनीति से लेकर समाज तक, यह दोहरापन हर जगह देखने को मिलता है—जहां लोग अपनी सुविधानुसार सिद्धांत और मुखौटे बदलते रहते हैं। इस रचना के माध्यम से आज के दौर के ‘नए क्रांतिवीरों’ की सच्चाई को बेनकाब करने का प्रयास किया गया है।
कल जो हमारे गले पर छुरी चलाने में एक पल भी नहीं हिचके, आज वही लोग न्याय की गद्दी पर बैठकर हमारे लिए न्याय की मिसालें गढ़ रहे हैं। समय ने उनके चेहरे को इतना बदल दिया है कि मानो रंग बदलने वाले गिरगिट से भी तेज हो गए हों। कल तक जिनकी आंखों से खून टपकता था, आज उनकी आंखों से शांति के पैगाम निकल रहे हैं। वही हाथ जो कल तलवारें लहरा रहे थे, आज सफेद झंडे फहराते हैं, शांति के कपोत उड़ाते हैं, और लोग हैं कि वाह-वाह किए बिना रह नहीं पाते।
अब देखिए न, उन्हीं लोगों ने कल तक जलते हुए शहरों में आग लगाने का काम किया, और आज वे फायर ब्रिगेड के हीरो बन गए हैं। कभी पेट्रोल की बोतलें लिए घूमते थे, आज पानी के पाइप लेकर आग बुझाने निकल पड़े हैं। मानो उनकी जिंदगी का मकसद ही ‘बचाने का नया खेल’ बन गया हो।
किसी को याद भी है कि कल तक इन्हीं के हाथों बस्तियों का नामोनिशान मिटा दिया गया था। चारों तरफ तबाही का मंजर था—घोंघे, पत्थर, और कूड़ा-कर्कट बिखरा पड़ा था। और हां, कुछ सरकटी लाशें भी वहीँ पड़ी थीं। लेकिन अब वक्त बदला है, और वक्त के साथ ये लोग भी बदल गए हैं। कल जो ‘भारत माता की जय’ चिल्लाते हुए एक-दूसरे की पीठ में छुरे घोंप रहे थे, आज वही लोग घायलों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं।
दंगों की आग अब बुझ चुकी है, और अब ये महाशय सम्मान पत्र बांटने और अपना अभिनंदन खुद करवाने में जुट गए हैं। कहते हैं, “हमने इन दंगों के दर्द को अपनी आत्मा पर झेला है!” वाह! मानो कि कोई बड़ी तपस्या कर डाली हो। जबकि सच तो यह है कि इसी तपस्या के बहाने उन्होंने पानी की एक बाल्टी भी दोगुने दाम पर बेची। और अब इसे ‘मानव सेवा’ के नाम पर गिनाते हैं।
जो कल तक “खून का बदला खून” चिल्लाते थे, आज वही लोग सूरजमुखी की तरह मुड़कर शांति के सूरज का स्वागत कर रहे हैं। समय की चाल को भांपते हुए, ये लोग तो ‘गंगा गए तो गंगाराम’ और ‘जमना गए तो जमनादास’ बनने में माहिर हो चुके हैं। आजकल यह कला इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि राजनीति के बाज़ार में ‘दलबदलू’ की पदवी भी इन्हें शर्मिंदा नहीं करती। यह तो उनके लिए एक ‘आत्मावलोकन’ का प्रतीक बन चुका है।
अब हाल यह है कि दलबदलू कानून भी इनकी राह नहीं रोक पाते। गठजोड़ संस्कृति का ऐसा चलन चल पड़ा है कि चुनावी भाषणों में एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, चुनाव के बाद एक-दूसरे के गले लग जाते हैं। सत्ता की मिठाई बांटने का काम हो, या न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर मुहर लगानी हो, सब कुछ चुटकियों में निपटा लिया जाता है।
विभिन्न विचारधाराओं के ‘पुरोधा’ भी देखते-देखते एक ही मंच पर आ जाते हैं। और फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर, इसे एक नई क्रांति की शुरुआत घोषित कर देते हैं।
कहानी का सार यही है कि इस राजनीति के बाजार में सब कुछ बिकाऊ है—मानवता से लेकर शांति के झंडे तक। और जो असल हकदार थे, वे पहचान और सम्मान के इस मेले में कहीं खो गए। अब यह देखना बाकी है कि अगले चुनाव में कौन-सा नया मुखौटा सामने आएगा।
शांति का ये नया बाजार है, जहां सिद्धांत और मूल्य कब अदल-बदल कर दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बस एक मुखौटा पहनिए और अगली सुबह का सूरज आपका इंतजार कर रहा है।

Author: जगदंबा उपाध्याय, मुख्य व्यवसाय प्रभारी
जिद है दुनिया जीतने की