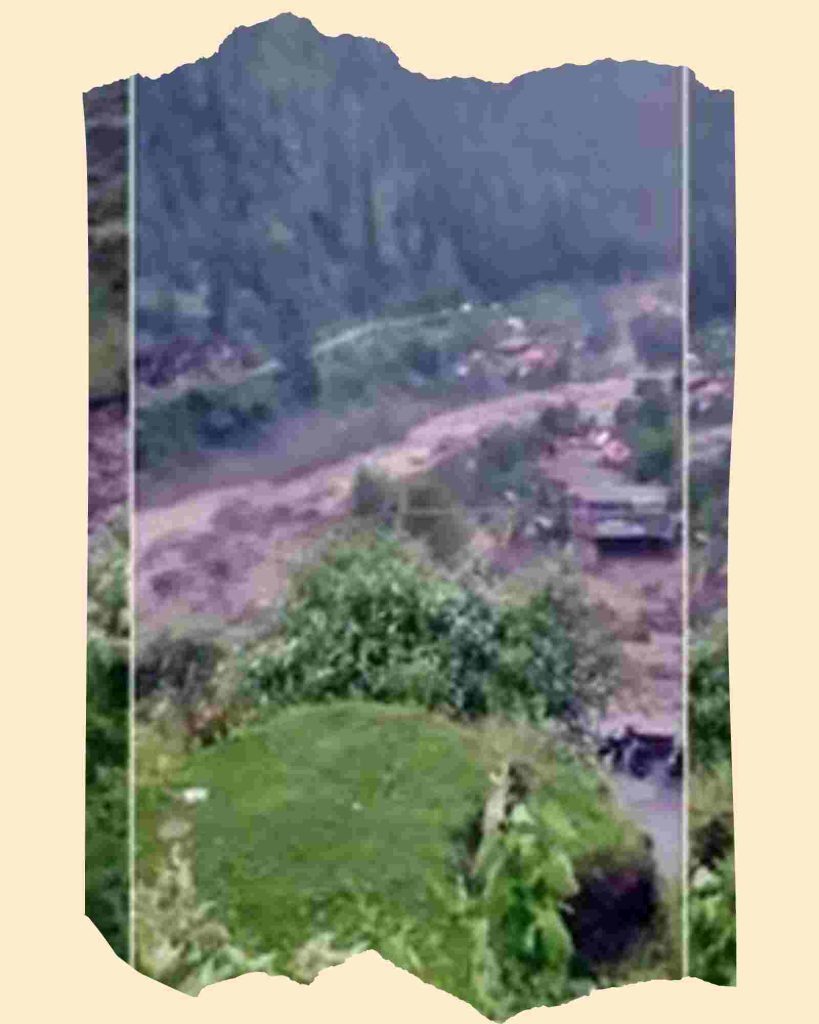
मोहन द्विवेदी की खास रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक तथा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के लिए विश्व-विख्यात है। हिमाचल प्रदेश का अधिकांश भाग सुंदर, सौम्य, गगनचुंबी पहाड़ों व कल-कल करती बहती नदियों के कारण हर किसी का मन मोह लेता है। लेकिन बरसात के महीनों में इन पहाड़ों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन तथा पानी का जलस्तर बढऩे के कारण अनेकों आपदाएं मानव जीवन को लील लेती हैं। 8, 9 तथा 10 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश में भयंकर बारिश हुई जिसके कारण प्रदेश को जान-माल के साथ करोड़ों रुपए का नुकसान भी झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा रौद्र रूप ब्यास नदी ने धारण किया। इसके समीप बसे कुल्लू से लेकर मंडी तक के स्थानीय जनमानस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुल्लू जिला में ब्यास नदी के समीप बने फोरलेन, अन्य मार्ग तथा स्थानीय लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं मंडी में वर्ष 1877 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए विक्टोरिया ब्रिज को भी इतिहास में पहली बार ब्यास नदी के जल ने छू लिया। पर्यटकों तथा व्यवसायियों को भी इस आपदा में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा।
वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन ने अपना क्रूर चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में 200 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। यही हाल उत्तराखंड का है। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर में जान-माल की अप्रत्याशित तबाही दिल दहला देने वाली है। मृतकों की संख्या 80 हो गई है। जगह-जगह लोग प्रकृति के क्रोध के शिकार हो कर असहाय अनुभव कर रहे हैं। सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, किन्तु साल दर साल बढ़ती बाढ़ की विभीषिका कई सवाल खड़े कर रही है। जलवायु परिवर्तन के असर की भविष्यवाणी तो कई सालों से की जा रही है और जिसके चलते हिमालय जैसे नाजुक पर्वत क्षेत्र में उचित सावधानियां क्यों नहीं उठाई गई हैं। सैंकड़ों पर्यटक जगह जगह फंसे पड़े हैं। ईश्वर का शुक्र है कि सब सुरक्षित हैं। सरकार भी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्रवाई कर रही है, किन्तु बरसात में पर्यटन को किस तरह दिशा निर्देशित किया जाना चाहिए, इस बात की कमी खलती है। पर्यटन सूचना केन्द्रों का नेटवर्क सक्रिय होना चाहिए जो बरसात के खतरों से अवगत करवाए। मंडी में हुई तबाही के पीछे लारजी और पंडोह बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बांधों के निर्माण के समय बाढ़ नियंत्रण में बांधों की भूमिका का काफी प्रचार किया जाता रहा है, किन्तु देखने में तो उल्टा ही आ रहा है। बांधों से अचानक और बड़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी ही अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनता जा रहा है।
हालांकि इस विषय पर चर्चा तो सरकारी क्षेत्रों में चलती रहती है, वर्तमान सरकार में भी नीति आयोग द्वारा हिमालयी क्षेत्र में विकास की दिशा तय करने के लिए रीजनल कौंसिल का गठन किया गया है, किंतु अभी तक इस संस्था की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। अब समय है कि सब नींद से जागें और हिमालय में विकास की गतिविधियों को प्रकृति मित्र दिशा देने का प्रयास करें। हमें सोचना होगा कि हिमालय में होने वाली कोई भी पर्यावरण विरोधी कार्रवाई पूरे देश के लिए हिमालय द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं से वंचित करने वाली साबित होगी…
वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन ने अपना क्रूर चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में 200 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। यही हाल उत्तराखंड का है। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर में जान-माल की अप्रत्याशित तबाही दिल दहला देने वाली है। मृतकों की संख्या 80 हो गई है। जगह-जगह लोग प्रकृति के क्रोध के शिकार हो कर असहाय अनुभव कर रहे हैं। सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, किन्तु साल दर साल बढ़ती बाढ़ की विभीषिका कई सवाल खड़े कर रही है। जलवायु परिवर्तन के असर की भविष्यवाणी तो कई सालों से की जा रही है और जिसके चलते हिमालय जैसे नाजुक पर्वत क्षेत्र में उचित सावधानियां क्यों नहीं उठाई गई हैं। सैंकड़ों पर्यटक जगह जगह फंसे पड़े हैं। ईश्वर का शुक्र है कि सब सुरक्षित हैं। सरकार भी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्रवाई कर रही है, किन्तु बरसात में पर्यटन को किस तरह दिशा निर्देशित किया जाना चाहिए, इस बात की कमी खलती है। पर्यटन सूचना केन्द्रों का नेटवर्क सक्रिय होना चाहिए जो बरसात के खतरों से अवगत करवाए। मंडी में हुई तबाही के पीछे लारजी और पंडोह बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बांधों के निर्माण के समय बाढ़ नियंत्रण में बांधों की भूमिका का काफी प्रचार किया जाता रहा है, किन्तु देखने में तो उल्टा ही आ रहा है। बांधों से अचानक और बड़ी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी ही अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनता जा रहा है।
बरसात से पहले बांधों में बाढ़ का पानी रोका जा सके, इसके लिए बांधों को खाली रखा जाना चाहिए, किन्तु अधिक से अधिक बिजली पैदा करने के लिए बांध भरे ही रहते हैं। बरसात आने पर पानी जब बांध के लिए खतरा पैदा करने के स्तर तक पहुंचने लगता है तो अचानक इतना पानी छोड़ दिया जाता है जितना शायद बिना बांध के आई बाढ़ में भी न आता। इन मुद्दों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बांध प्रशासन को निर्देशित किया जाना चाहिए। बांधों की बाढ़ नियंत्रण भूमिका को सक्रिय किया जाना चाहिए। दूसरा बड़ा गड़बड़ सडक़ निर्माण में हो रही लापरवाही से भी हो रहा है। निर्माण कार्य में निकलने वाले मलबे को निर्धारित स्थानों, डंपिंग स्थलों में न फेंक कर यहां-वहां फेंक दिया जाता है और वही मलबा बाढ़ को कई गुणा बढ़ाने का कारण बन जाता है। मलबा जब एक बार नीचे ढलानों पर खिसकना शुरू होता है तो अपने साथ और मलबा बटोरता जाता है, जिससे भारी तबाही का मंजर पेश हो जाता है। नदी-नालों में जब यह मलबा पहुंचता है तो नदी का तल ऊपर उठ जाता है और वे क्षेत्र जो पहले कभी बाढ़ की जद में नहीं आए थे, वे भी अब बाढ़ की जद में आ जाते हैं। सडक़ निर्माण में जल निकासी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। सडक़ किनारे बनाई गई नालियों से जल इकट्ठा होकर कहीं एक जगह छोड़ दिया जाता है जो भू-कटाव को बढऩे का कारण बनता है। सडक़ निर्माण विधिवत पर्वतीय दृष्टिकोण से कट एंड फिल तकनीक से किया जाना चाहिए। पहाड़ों में सडक़ के विकल्पों पर भी सोचा जाना चाहिए। सडक़ तो जीवन रेखा है, किन्तु जीवन रेखा यदि जीवन को ही लीलने लग जाए तो सोचना पड़ेगा कि गड़बड़ कहां हो रही है। सडक़ के विकल्प के रूप में मुख्य मार्गों से लिंक सडक़ों के बजाय उन्नत तकनीक के रज्जू मार्ग बनाए जा सकते हैं, किन्तु इस दिशा में सरकारों ने सोचना ही शुरू नहीं किया है। हां, पर्यटन आकर्षण के रूप में कुछ कुछ जगहों में रज्जू मार्ग बने हैं। उनके अनुभव से सस्ती और टिकाऊ यातायात सुविधा निर्माण की जा सकती है।
फिलहाल जब यह बात उजागर हो गई है कि मलबा डंपिंग की भूमिका भूस्खलन बढ़ाने में मुख्य है तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि इसका सुओ-मोटो संज्ञान लेकर जहां जहां नुकसान हुआ है वहां तकनीकी जांच करवाई जाए। राष्ट्रीय राज मार्गों के मामले में चीफ विजिलैंस अफसर राष्ट्रीय राजमार्ग को जांच के लिए कहना चाहिए। 1994 में भागीरथी के तट पर, जब टिहरी बांध विरोधी आन्दोलन चल रहा था, तब हिमालय बचाओ आन्दोलन का घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसकी मुख्य मांग थी कि हिमालय की नाजुक परिस्थिति के मद्देनजर हिमालय के लिए विकास की विशेष प्रकृति मित्र योजना बनाई जाए। योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए डा. एस. जेड. कासिम की अध्यक्षता में बनाई गई विशेष समिति ने भी 1992 में इसी आशय की रिपोर्ट जारी की थी, किन्तु उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों के लोग लगातार विकास के नाम पर चल रही अंधी दौड़ के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, किन्तु सरकारों और तकनीकी योजना निर्माताओं के कानों में जूं भी नहीं रेंगती है। एक अच्छा बहाना इन लोगों को मिल जाता है कि प्रकृति के आगे हम क्या कर सकते हैं, किन्तु इन लोगों को पूछा जाना चाहिए कि प्रकृति को इतना मजबूर करने का आपको क्या हक है कि प्रकृति बदला लेने पर उतारू हो जाए। हालांकि इस विषय पर चर्चा तो सरकारी क्षेत्रों में चलती रहती है, वर्तमान सरकार में भी नीति आयोग द्वारा हिमालयी क्षेत्र में विकास की दिशा तय करने के लिए रीजनल कौंसिल का गठन किया गया है, किन्तु अभी तक इस संस्था की कोई गतिविधि सामने तो नहीं आई है। अब समय है कि सब नींद से जागें और हिमालय में विकास की गतिविधियों को प्रकृति मित्र दिशा देने का प्रयास करें। हमें सोचना होगा कि हिमालय में होने वाली कोई भी पर्यावरण विरोधी कार्रवाई पूरे देश के लिए हिमालय द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवाओं से वंचित करने वाली साबित होगी।
आखिरकार हिमाचल प्रदेश में पिछले एक दशक से प्राकृतिक आपदाएं बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। इसके कुछ कारणों का भी पता लगाना समय की सबसे बड़ी मांग बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में दो वर्षों में भूस्खलन के मामलों में छह गुना वृद्धि दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2020 में भूस्खलन के महज 16 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में यह मामले छह गुना बढक़र 117 हो गए। विभाग के मुताबिक राज्य में 17120 भूस्खलन संभावित स्थल हैं, जिनमें से 675 स्थल महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और बस्तियों के पास हैं। ये स्थल चंबा (133), मंडी (110), कांगड़ा (102), लाहौल और स्पीति (91), ऊना (63), कुल्लू (55), शिमला (50), सोलन (44), बिलासपुर (37), सिरमौर (21) और किन्नौर (15) में हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, कुल्लूृ, ऊना, मंडी, सिरमौर और शिमला जिले फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, बादलों के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति तथा किन्नौर में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हर वर्ष प्रदेश सरकार तथा आम जनमानस को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ती भूस्खलन की घटनाओं का विश्लेषण करना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान समय में हिमाचल के लोगों का रहन-सहन, खानपान, आवागमन तथा पहनावा आधुनिकता की चकाचौंध का मोहताज होता जा रहा है। आज प्रदेश के पहाड़ों को कुछ चंद जरूरतों को पूरा करने के लिए बेरहमी से कुरेदा जा रहा है।
प्रदेश में असंख्य हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, फोरलेन का निर्माण तथा हर गांव, कस्बे, शहर में पहाड़ों को चीरने-फाडऩे की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। हर कोई इन पहाड़ों को चीर करके अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने में लगा है। सरकार इस प्रक्रिया को विकास का नाम देती है, वहीं आम जनता इस प्रक्रिया को अपनी सुख-सुविधाओं की बुनियादी जरूरत बताती है। जब पहाड़ों के बीच से सडक़ मार्ग, हाइड्रो प्रोजेक्ट तथा सुरंगों के निर्माण के दौरान अत्यधिक विस्फोट किए जाते हैं जिससे पहाड़ जर्जर हो जाते हैं और बरसात के समय में जब उनमें थोड़ा सा पानी अंदर घुसता है तो वे भूस्खलन का रूप धारण करके प्रदेश के जनमानस के लिए आपदा पैदा करते हैं। इस समस्या को एक अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ी सरलता से समझने में सक्षम है। लेकिन इस प्रदेश के कर्णधार इस बात को समझने के लिए कतई भी राजी नहीं हैं। इन पहाड़ों को कुरेदने से अच्छा होता आवागमन के अन्य विकल्पों को तलाशा जाता तथा पहाड़ों के साथ कम से कम छेडख़ानी की जाती। हिमाचल प्रदेश में रेल मार्ग, जल मार्ग तथा हवाई मार्ग के निर्माण को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन प्रदेश के कर्णधार सडक़ मार्ग पर ही अटल हैं, जिसके परिणाम घातक साबित हो रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ कहीं न कहीं आज मानव जीवन के समक्ष अनेकों मानव जनित समस्याओं को उजागर कर रही है। वर्तमान समय में प्रदेश का जनमानस ऐसी परिस्थिति में आ गया है जहां पर उसे सिर्फ अपना जीवन सुरक्षित करना ही सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में न तो विकास के इन मसीहाओं को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, न ही बढ़ते जलवायु संकट को दोषी ठहराया जा सकता है। जितना हो सके, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए यथासंभव सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच करें अन्यथा प्रदेश का जनमानस अपनी जान से हाथ धोता रहेगा। दो दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां, 4 दिन प्रदेश के नेताओं की शोक संवेदनाएं तथा 13 दिन तक रिश्तेदारों तथा धर्म कांड का प्रचलन देखने को मिलेगा।
उसके बाद ताउम्र के लिए आपके परिवार को घाव मिलेंगे। यह जीवन का आधारभूत सत्य है, इसे स्वीकार करना ही होगा। 21वीं सदी के मानव ने अनेकों सूचना प्रौद्योगिकी के यंत्रों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से जनमानस को बचाने की अनेकों नवीन तरीके इजाद किए हैं। इस कड़ी में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा भूस्खलन की जानकारी देने वाला सेंसर वार्निंग सिस्टम इजाद किया है, जोकि भूस्खलन की घटनाओं से सूचित करने में सहायक साबित है। इस सिस्टम के माध्यम से अनेकों जनमानस की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसके साथ सरकार को, प्रदेश में अवैज्ञानिक व अवैध खनन किसी भी सूरत पर न हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। पर्यावरणविदों के इस विचार पर भी गौर करना समय की मांग बन चुका है कि हिमालय के इलाकों में, खासतौर से सतलुज और चिनाब घाटी में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इनसे पडऩे वाले दुष्प्रभावों पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
