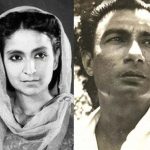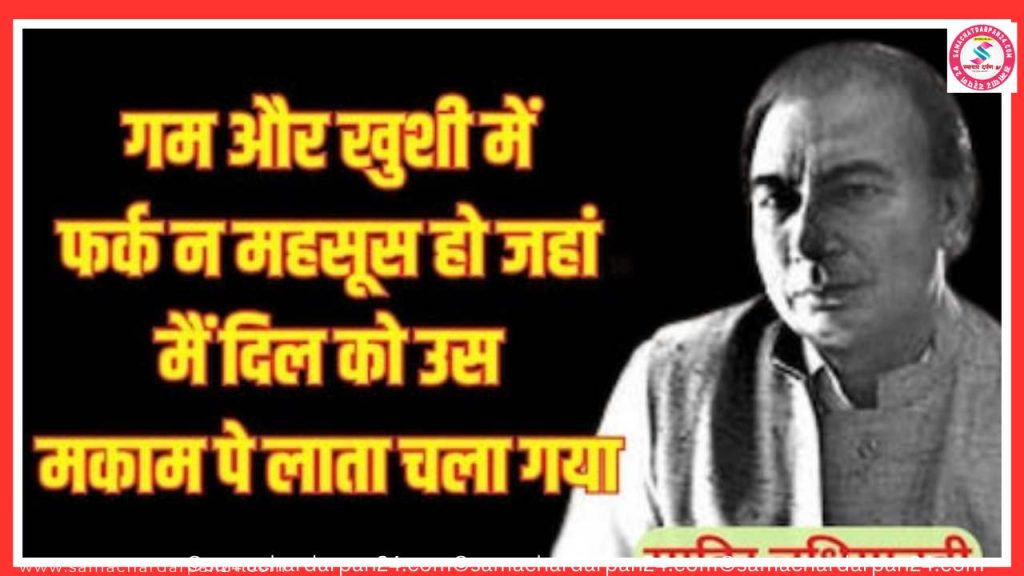
अनिल अनूप
साहिर लुधियानवी (Sahir Ludhianvi) हिंदी सिनेमा के बड़े नग़्मा-निगारों में से एक थे। जिस समय उनका गीत लेखन के क्षेत्र में आगमन हुआ वह दौर भारी हंगामाखेज था, चारों तरफ तक़्सीम की त्रासदी पसरी हुई थी। इंसानियत को शर्मसार करने की कोई कोर-कसर नहीं बची थी। साथ ही आलमी सतह पर दूसरी जंग-ए-अज़ीम (विश्वयुद्ध) की विभीषिका भी दुनिया के सामने थी। तबाही का ऐसा मंज़र दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस दौर की त्रासदी, साहिर की ज़ाती पीड़ा यानी ग़म-ए-हयात में पैवस्त होकर उनके गीतों में हमेशा नमूदार होती रही।
साहिर ने खुद कहा भी – दुनिया ने तजरबात ओ हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं ।
साहिर अकेले ऐसे गीतकार हुए जिनके गीत उस पूरे माशरे की तर्जुमानी करते हैं।
साहिर के गीतों में एक इंसान के अंदर की कशमकश, उसके अंदर की आग, बग़ावत और फिर वही मामूली आदमी की बेबसी कहीं न कहीं दिख ही जाती है। हालांकि उस समय कई बडे शायर फ़िल्मी गीत लेखन के क्षेत्र में आए, फ़िल्मों में आने से पहले उनकी शायरी में भी वही कैफ़ियत, जज़्बात की तपिश, तरक़्क़ीपसंदी थी। लेकिन कुछेक मौकों को छोड़कर उनके फ़िल्मी गीतों में वह कैफ़ियत नहीं दिखी जो ताउम्र साहिर के गीतों में रही। कई शायरों को तो सिनेमा की दुनिया रास ही नहीं आई।
रूमानियत का रंग
फ़िल्मी गीतकारों में साहिर की रूमानियत का रंग औरों से जुदा था। उनके यहां रूमानियत थी – कभी न ठंडी पड़ने वाली मद्धिम आंच की तरह। उनकी रूमानियत के तेवर बग़ावती तो थे ही, उसमें अजीब सी नीम-उदासी, नॉस्टैल्जिया का रंग भी था, साथ ही उसमें कुदरती नीरवता, स्वप्नशीलता और विह्वलता थी। मिसाल के तौर पर फ़िल्म धर्मपुत्र (1962) के इस गीत को देखिए:
मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो
और झाँक के मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो …
भारत में कई ऐसे शायर हुए हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। उनमें से एक साहिर लुधियानवी है। ऐसा अक्सर शायर लोग करते थे जो जिस शहर के होते अपने नाम के आगे उस शहर का नाम जोड़ लेते थे।
ऐसा माना जाता है कि साहिर लुधियानवी उस दौर की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम से प्यार करते थे लेकिन उनकी कहानी अधूरी रह गई। जिस वजह से साहिर लुधियानवी ने लंबा विराम लिया और फिर ऐसे-ऐसे गाने लिखे जो सदाबहार बन गए। चलिए आपको साहिर और अमृता से जुड़ा एक मशहूर किस्सा बताते हैं।
क्यों अधूरी रही साहिर लुधियानवी की प्रेम कहानी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में उनकी लव स्टोरी मशहूर हुआ करती थी। साहिर शुरू से ‘नज्में’ और ‘गजलें’ लिखा करते थे जिसके कारण कॉलेज में वो मशहूर थे। अमृता प्रीतम भी उन्हें इसी वजह से ज्यादा पसंद करती थीं। टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमृता को साहिर पसंद थे लेकिन उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम से प्यार करे। बाद में साहिर को उक कॉलेज से अमृता के पिता के कहने पर निकाला गया। साहिर ने पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ छोटी-मोटी नौकरियां की और साल 1943 में लाहौर आ गए।
यहां पर साहिर ने संपादक के तौर पर काम किया और इसी मैगजीन में एक ऐसी रचना छापी जिसे पाकिस्तान के विरुद्ध माना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तभी साहिर को भारत वापस भेजने के लिए फोर्स किया गया और साल 1949 में साहिर भारत आ गए। साहिर लुधियानवी ने शादी नहीं की, हालांकि उनकी लाइफ में एक और महिला सुधा मल्होत्रा आईं लेकिन साहिर का वो रिश्ता भी सफल ना हुआ।
मशहूर कवि साहिर लुधियानवी का जन्म 1921 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनका असली नाम अब्दुल हई फजल मोहम्मद था। उनके पिता चौधरी फजल मोहम्मद सिखेवाल के एक धनी जमींदार थे और गुज्जर समुदाय से थे। जब वह मुश्किल से छह महीने के थे, उनके माता-पिता अलग हो गए और उनकी मां सरदार बेगम ने बच्चे अब्दुल को अपने साथ लेकर घर छोड़ दिया। 8 मार्च को साहिर की बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर आपको बताते हैं कि वो कौन सी कविता थी जिसकी वजह से उन्हें लाहौर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही, उनकी मां से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं।
Sahir Ludhianvi को कम उम्र से ही कविता पढ़ने और लिखने दोनों में रुचि हो गई। मौलाना फ़ैज़ हरियाणवी के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी का सीखा और जल्द ही इन भाषाओं में पारंगत हो गए। इक़बाल के एक दोहे में, उन्हें साहिर शब्द मिला, जिसका अर्थ जादूगर होता है और उन्होंने इसे अपने सरनेम के रूप में ले लिया। साहिर देश की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को लेकर चिंता में रहते थे और उन्होंने छात्र आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, कई सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में गए। वह 1943 में लुधियाना छोड़कर लाहौर चले गए और दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां उन्हें छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। यही वो जगह थी जहां से साहिर में कवि बनने का हुनर पनपा।
लाहौर छोड़ने पर मजबूर हुए थे साहिर लुधियानवी
स्वतंत्रता के बाद, वह भारत में बस गए और फिल्मी गानों को लिखने लगे। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में उनका निधन हो गया। 1949 में, लाहौर में रहते हुए, साहिर लुधियानवी ने एक क्रांतिकारी कविता, ‘आवाज़-ए-आदम’ (द वॉयस ऑफ मैन) लिखी, जिसमें ‘हम भी देखेंगे’ एक यादगार लाइन बन गई। पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका को यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था कि वह उसकी साम्यवाद विरोधी नीति में मदद करेगा। पाकिस्तान खुद को बस साबित करने में लगा हुआ था।
और फिर कभी भारत से नहीं लौटे…
लेकिन साहिर की ये कविता प्रकाशित होने के बाद उन्हें ख़ुफ़िया एजेंसियों ने धमकी दी और मजबूर होकर वह भारत चले आये। उसके बाद साहिर ने ‘हम भी देखेंगे’ लिखी, जो उनकी पाकिस्तान से विदाई के रूप में याद की जाती है। उन्होंने यह कविता 1949 में लाहौर की एक सभा में पढ़ी और कुछ दिनों बाद भारत आ गए लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे।
मां की जिंदगी पर लिखी कविता
साहिर का कई महिलाओं के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन वह किसी भी महिला से उतना प्यार नहीं करते थे जितना वह अपनी मां सरदार बेगम से करते थे। उन्होंने अपने पति फजल दीन को छोड़ दिया था और साहिर को अकेले पाला था, जिससे साहिर को फिल्म ‘त्रिशूल’ (1978) में ‘तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने’ लिखने के लिए प्रेरणा मिली। साहिर ने इस कविता में अपनी मां की पूरी जिंदगी लिख दी, जिसमें साहिर की मां को उस परेशानी का सामना करना पड़ा था, जब साहिर को छोड़ने के बाद उनके पति ने साहिर की कस्टडी के लिए उन्हें परेशान किया था।
उदासी का कैनवास
साहिर के फ़िल्मी गीतों में पसरी उदासी का कैनवास इतना बड़ा है कि ज़ाती उदासी आलमी उदासी में तब्दील होती दिखाई देती है। हिन्दी फ़िल्मों में शायद ही ऐसा रंग किसी और के यहां मिले। फ़िल्मों से इतर यह रंग सबसे ज्यादा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के यहां है। उदासी के ये रंग आप फ़िल्म प्यासा (1957) के गीतों में देख सकते हैं। मसलन-
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है…, जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहां हैं…,जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला…, तंग आ चुके हैं कशमकश-ए-ज़िंदगी से हम… ।
बोल सरल लेकिन महज तुकबंदी नहीं
सिचुएशन और कैरेक्टर के हिसाब से इनके गीतों के बोल कहीं सरल हैं लेकिन वहां भी महज तुकबंदी, सपाटबयानी नहीं है। सरलता और मायने दोनों देखना हो तो, बानगी के तौर पर फ़िल्म फिर सुबह होगी (1958) का यह गीत देखिए:
दो बूँदे सावन की…
इक सागर की सीप में टपके और मोती बन जाये
दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाये
किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाये
सियासी सोच का फ़लक
साहिर की अपने माशरे (दौर) पर हमेशा पैनी नजर रही। जब तक एक गीतकार को अपने माशरे की व्यापक समझ नहीं होगी तब तक वह एक साथ अलग अलग सिचुएशन और कैरेक्टर के लिए गीत नहीं लिख सकता। मतलब वह एक सफल गीतकार नहीं हो सकता।
उनकी सियासी सोच का फ़लक भी काफी बड़ा था, जिसमें हर तरह के मौज़ूआत शामिल थे। वे घोषित मार्क्सवादी तो थे ही, साथ साथ एक गांधीवादी भी थे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उनके गीत हैं। फिल्म नया दौर (1957) के गीतों को लीजिए, जो पूरी तरह से गांधीवादी और समाजवादी सोच की तर्जुमानी करते हैं।
साहिर एक हद तक आदर्शवादी भी थे। जिसे आप उनकी मानवतावादी सोच से भी जोड़ सकते हैं। उन्हें हिंदोस्तान की गंगा-जमुनी तहज़ीब की गहरी समझ थी। तभी तो बच्चे की मासूमियत के जरिए फिरकों में बंटी इस दुनिया पर जैसा तंज़ फ़िल्म ‘धूल का फूल’ के गीत …. तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा….में है, शायद ही इसकी कोई दूसरी मिसाल हो। इस गीत के अंतरे यानी बंद को देखिए, किस तरह से मज़हबी सियासत के नापाक मंसूबों को बेनक़ाब करती है-
अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है
तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं है
जिस इल्म ने इंसान को तक़सीम किया है
उस इल्म का तुझ पर कोई इलज़ाम नहीं है………
दुख का रंग भी साहिर के यहां यकसां नहीं था। उनके अंदर इंसानी तकलीफ और बेचैनी को पढने का गजब शऊर था। व्यवस्था और समाज के दोहरेपन, विसंगतियों और खोखलेपन पर साहिर ने अपने फ़िल्मी गीतों के जरिए जमकर प्रहार किया, जिसकी सबसे बडी मिसाल उनकी फ़िल्म प्यासा है।
कहें तो हर एहसास/मानवीय संवेदना को उन्होंने पढ़ने की, बुनने की भरपूर कोशिश की। इतने बडे/विविध एहसासात को गीतों में उतारने के लिए उनके पास लफ़्ज़ों का ज़ख़ीरा भी था।