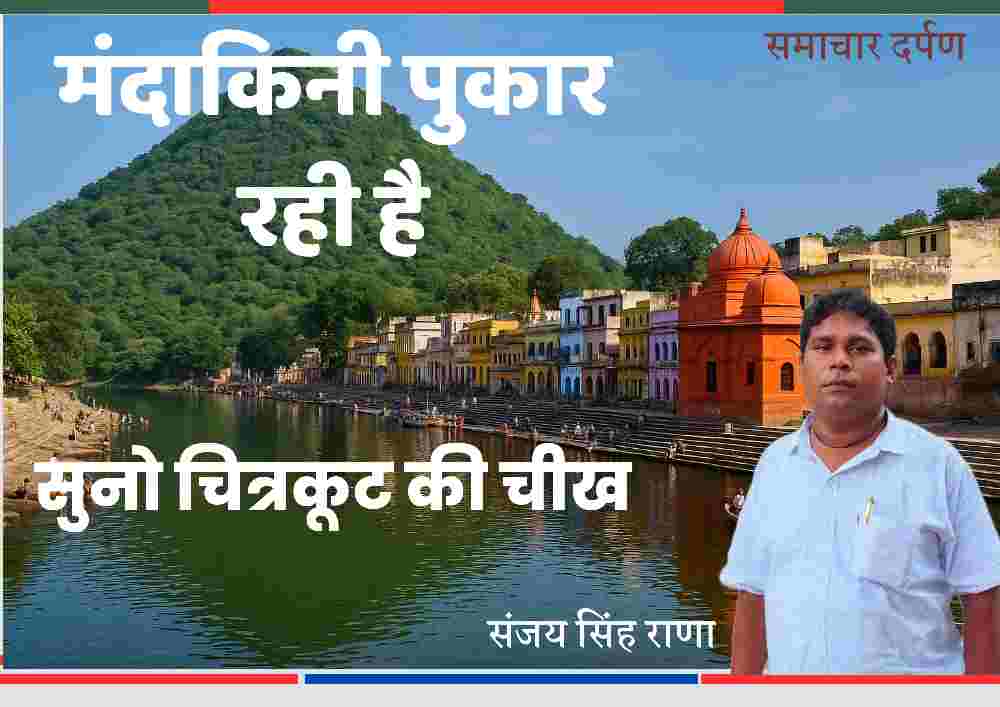
संजय सिंह राणा की रिपोर्ट
बुंदेलखंड का चित्रकूट जिला आज उस मोड़ पर खड़ा है, जहाँ से या तो वह अपने भूगोल, जंगलों और नदियों को बचाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकता है,
या फिर धीरे-धीरे सूखे, गर्मी, खनन और प्रदूषण की मार से अपनी पहचान खो बैठने की ओर बढ़ सकता है।
कभी पहाड़ों की हरियाली, मंदाकिनी की निर्मल धारा और घने वनों के लिए पहचाना जाने वाला यह क्षेत्र अब जलसंकट, बढ़ते तापमान, घटते जंगल और अनियंत्रित खनन के कारण
गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है।
यह स्थिति केवल प्रकृति की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों, स्थानीय समाज, खेती-किसानी और धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व पर सीधा हमला है।
इसलिए चित्रकूट के भौगोलिक परिदृश्य को समझते हुए उसके संरक्षण की स्पष्ट, ठोस और तात्कालिक रणनीति बनाना अनिवार्य हो गया है।
1. चित्रकूट का भूगोल : प्रकृति की विविधता का संगम
चित्रकूट की भू–रचना केवल नक्शे पर दर्ज कुछ रेखाएँ भर नहीं है, बल्कि पहाड़ों, पठारों, नदी घाटियों और घने वनों का ऐसा संतुलन है,
जो पूरे जिले की जलवायु, खेती, संस्कृति और जीवन शैली को निर्धारित करता है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के प्रभाव से बना यह भूभाग
प्राकृतिक विविधता से भरा हुआ है, लेकिन यही विविधता आज मानवीय दबाव की सबसे बड़ी शिकार भी है।
1.1 पहाड़ी और पठारी भू-आकृति
चित्रकूट का अधिकांश हिस्सा चट्टानी पहाड़ियों और पठारी भूमि से बना है। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी सिरे और विंध्य क्षेत्र की
संरचनाएँ यहाँ की पहाड़ियों को विशिष्ट बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ मुख्यतः कठोर चट्टानों, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित हैं,
जो हजारों-लाखों वर्षों के भूगर्भीय परिवर्तन का परिणाम हैं।
इन पहाड़ियों की सबसे बड़ी भूमिका भूजल पुनर्भरण और जल–संचयन में है। मानसून के समय जब वर्षा का पानी इन ढलानों पर गिरता है, तो चट्टानी प्रकृति के कारण
यह पानी सीधे गहराई तक नहीं समाता, बल्कि ढलानों के सहारे नीचे की तरफ बहता हुआ प्राकृतिक तालाबों, नालों और खेतों तक पहुँचता है।
यही प्रक्रिया चित्रकूट के जल–तंत्र को जीवित रखती है। लेकिन जब इन्हीं पहाड़ियों पर अंधाधुंध खनन, सड़क कटान या निर्माण कार्य बढ़ते हैं,
तो ढलान की यह प्राकृतिक संरचना टूटने लगती है और बरसात का पानी सीधे तेज़ी से बहकर निकल जाता है, जिसके कारण जलस्रोतों की भराव क्षमता घट जाती है।
1.2 नदियाँ और जलधाराएँ
चित्रकूट की जीवनरेखा मानी जाने वाली मंदाकिनी नदी के बिना इस क्षेत्र के भूगोल की कल्पना भी अधूरी है। इसके अलावा तमसा, पयस्विनी और कई छोटी–बड़ी बरसाती धाराएँ
पूरे जिले में जल का वितरण करती हैं। कभी इन नदियों का प्रवाह सालभर बना रहता था, लेकिन अब लंबे समय तक सूखी धाराएँ और उथली होती जलधारा एक आम दृश्य बनती जा रही हैं।
नदियों के किनारों पर अतिक्रमण, घाटों के आसपास अनियोजित निर्माण, सीवेज का बहाव, प्लास्टिक और कचरे का ढेर—ये सब मिलकर जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को प्रभावित कर रहे हैं।
वन कटान के कारण वर्षा जल का धीरे-धीरे रिसकर नदी में पहुँचने की प्रक्रिया कमजोर हुई है, फलस्वरूप बरसात के बाद नदी का जलस्तर तेजी से गिरने लगता है।
यह केवल धार्मिक या पर्यटक की दृष्टि से समस्या नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के जलविज्ञान पर गंभीर प्रहार है।
1.3 वन और जैव-विविधता
चित्रकूट के जंगल कभी इस क्षेत्र की पहचान हुआ करते थे। महुआ, सागौन, खैर, अर्जुन, अंजीर, सेमर और अनेक स्थानीय वृक्ष प्रजातियाँ इन वनों की रीढ़ हैं।
इन जंगलों में चिंकारा, नीलगाय, खरगोश, लोमड़ी, मोर, तीतर और कई प्रकार के पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं, जो यहाँ की जैव-विविधता को समृद्ध बनाते हैं।
वनों की यह हरियाली ही बारिश के पैटर्न को स्थिर रखती है, तापमान नियंत्रित करती है, मिट्टी को बिखरने से बचाती है और भूजल के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है।
जैसे-जैसे लकड़ी, चारा, ईंधन और खेती के लिए जंगल काटे गए, वैसे-वैसे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत तेजी से बहने लगी। पहाड़ियों का हरापन कम हुआ, चट्टानी भूमि बढ़ी,
और गर्मियों में तापमान लगातार ऊपर जाने लगा। यह सब मिलकर चित्रकूट को एक जल-संकटग्रस्त और पर्यावरणीय संकट से जूझते भूभाग के रूप में बदल रहे हैं।
2. जलविज्ञान : एक संवेदनशील जल–तंत्र पर बढ़ता दबाव
चित्रकूट की जल–व्यवस्था पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। औसतन 800–900 मिमी के आसपास वर्षा तो होती है, लेकिन वह भी मुख्यतः कुछ ही महीनों में सिमट जाती है।
इसके बाद लंबे समय तक पड़ने वाली तेज गर्मी और सूखा पूरे जल–तंत्र पर असमान दबाव डालते हैं।
2.1 जलस्रोतों का सिकुड़ना
तालाब, सरोवर, पहाड़ी कुंड और छोटे प्राकृतिक जलाशय गाँवों और शहरों के आसपास सदियों से जल का प्रमुख स्रोत रहे हैं।
लेकिन अब स्थिति यह है कि अधिकांश तालाब बरसात के कुछ महीनों बाद ही सूखने लगते हैं।
तालाबों में गाद भर जाने, चारों ओर अतिक्रमण, पक्के निर्माण, और नालों के रोक दिए जाने से उनकी जल–धारण क्षमता लगातार कम हुई है।
जहाँ पहले एक तालाब पूरे गाँव की प्यास बुझाता था, आज वह केवल बरसाती पोखर की तरह रह गया है।
नतीजा यह है कि पेयजल, सिंचाई और पशुओं के लिए पानी का संकट बढ़ता जा रहा है।
2.2 भूजल स्तर का गिरना
जब सतही जलस्रोत कमजोर हुए तो स्वाभाविक रूप से भूमिगत जल पर निर्भरता बढ़ी। नतीजतन हैंडपंप, नलकूप और बोरवेल की संख्या लगातार बढ़ती गई।
लेकिन recharge की व्यवस्था उतनी नहीं हुई, जितना दोहन हुआ।
पिछले वर्षों में कई ब्लॉक “ग्रे” या “क्रिटिकल” श्रेणी में पहुँच चुके हैं, जहाँ भूजल तेजी से नीचे जा रहा है।
गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाना, 25–30 फीट पर पानी न मिलना, किसानों को सिंचाई के लिए टैंकरों पर निर्भर होना—ये सब इस संकट के संकेत हैं।
यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में पेयजल के लिए लोगों को दूर-दूर तक भटकना पड़ सकता है।
2.3 बदलता मानसून और जल चक्र
जलवायु परिवर्तन का असर चित्रकूट के मानसून पर साफ दिखने लगा है। कभी बारिश समय पर और संतुलित होती थी, अब या तो देर से आती है, या कुछ दिनों में अत्यधिक हो जाती है।
अचानक होने वाली तेज बारिश से पानी रिसने के बजाय बहकर निकल जाता है, जिससे जमीन में जल भंडारण नहीं हो पाता। दूसरी ओर, लंबे शुष्क अंतराल के कारण मिट्टी सूखती है, फसलें झुलसती हैं और भूजल recharge नहीं हो पाता।
3. पर्यावरणीय संकट : टूटता हुआ प्राकृतिक संतुलन
3.1 अनियंत्रित खनन
मानिकपुर, भरतकूप और आसपास के क्षेत्रों में पत्थर खनन ने पहाड़ियों के प्राकृतिक स्वरूप को बुरी तरह प्रभावित किया है।
खनन से चट्टानें टूटती हैं, पहाड़ खोखले होते हैं, और बड़े पैमाने पर धूल–प्रदूषण फैलता है।
खदानों से निकली मिट्टी और पत्थर बारिश के दौरान नालों और तालाबों में भर जाते हैं, जिससे उनकी गहराई और जलधारण क्षमता घट जाती है।
खनन के ध्वनि–कंपन से कई बार आसपास की चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, जो गुफाओं, प्राकृतिक झरनों और छोटे जलस्रोतों के लिए घातक साबित होती हैं।
पहाड़ों का यह विनाश केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि जल, मिट्टी, वन, वन्यजीव और मानव जीवन सब पर एक साथ हमला है।
3.2 वनों की कटान
ईंधन, लकड़ी, चारा और खेती के विस्तार के लिए वर्षों से जंगल काटे जाते रहे हैं।
इस प्रक्रिया ने चित्रकूट के वन क्षेत्र को लगातार सिकोड़ दिया है।
जंगलों के घटने से सबसे पहले मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत प्रभावित होती है। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को थामे रखती हैं, उनके कटते ही वर्षा जल मिट्टी को बहा ले जाता है।
हरियाली कम होने से तापमान बढ़ता है, नमी घटती है और वर्षा का पैटर्न भी बदलने लगता है।
वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास से बेदखल होने लगते हैं और मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ भी बढ़ती हैं।
3.3 बढ़ता तापमान और सूखा
वन कटान, खनन और चट्टानी भूमि के विस्तार के कारण चित्रकूट का तापमान पिछले दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है।
गर्मी के दिनों में लू अधिक चलती है, रात का तापमान भी कम नहीं हो पाता और ठंडी हवाओं की जगह गर्म, सूखी हवाएँ चलती हैं।
जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, जलस्रोतों से पानी तेजी से उड़ने लगता है, मिट्टी की नमी खत्म होती है और फसलें झुलसने लगती हैं।
यह चक्र हर वर्ष और अधिक कठोर होता जा रहा है, जो चित्रकूट को एक सूखा–प्रवण क्षेत्र में बदलने की दिशा में धकेल रहा है।
3.4 पर्यटन का दबाव और प्रदूषण
धार्मिक पर्यटन चित्रकूट की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना प्रबंधन के यह पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है।
मंदाकिनी नदी के घाटों पर प्लास्टिक, पूजा सामग्री, खाद्य पैकेट, बोतलें और सीवेज का बहाव उसकी स्वच्छता और पवित्रता दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है।
घाटों के आसपास अनियोजित होटल–ढाबे, सीवेज ट्रीटमेंट की कमी और कूड़ा निस्तारण की कमजोर व्यवस्था ने नदी और आसपास के पर्यावरण पर भारी दबाव बनाया है।
यदि यही सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले समय में मंदाकिनी न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी गहरे संकट में पड़ सकती है।
4. सांस्कृतिक–भौगोलिक महत्व : जहाँ आस्था और प्रकृति एक-दूसरे से जुड़ी हैं
चित्रकूट का धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व उसके भूगोल से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ के अधिकांश तीर्थ–स्थल पहाड़ों, नदियों, गुफाओं और वनों से सीधे जुड़े हैं।
यानी यदि प्रकृति पर संकट आएगा तो आस्था के ये केंद्र भी सुरक्षित नहीं रह पाएँगे।
4.1 कामदगिरि पर्वत
कामदगिरि पर्वत को रामायणकालीन परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ की परिक्रमा मार्ग, आसपास की हरियाली और छोटी–छोटी जलधाराएँ इसका मूल आधार हैं।
यदि पर्वत की ढलानें कट जाएँ, पेड़ कम हो जाएँ या आसपास का क्षेत्र कंक्रीट से भर जाए, तो यह न केवल धार्मिक रूप से, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी गंभीर क्षति होगी।
4.2 गुप्त गोदावरी और प्राकृतिक गुफाएँ
गुप्त गोदावरी की गुफाएँ दो बड़े शिलाखंडों के बीच बहने वाली धारा के लिए प्रसिद्ध हैं। यह धारा पहाड़ियों के भीतर से रिसते जल के कारण बनती है।
यदि पहाड़ियों पर अत्यधिक खनन या कंपन हुआ, तो इन जलधाराओं का स्रोत कमजोर पड़ सकता है, जिससे गुफाओं का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है।
4.3 मंदाकिनी नदी
मंदाकिनी नदी की पवित्रता और स्थिर प्रवाह चित्रकूट की पहचान है। किन्तु घाटों पर बढ़ता कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक इसकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।
नदी को बचाना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के भूगोल और जल–तंत्र को बचाने की अनिवार्य शर्त भी है।
5. संरक्षण की आवश्यकता : क्यों कह रहा है चित्रकूट – अब नहीं तो कभी नहीं
5.1 भूजल संकट रोकने के लिए
यदि अभी संरक्षण पर गंभीर काम नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पानी की भारी कमी होगी।
भूजल स्तर का लगातार गिरना इस बात का संकेत है कि प्रकृति पर हमारी मांग उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा हो चुकी है।
5.2 नदियों और तालाबों के पुनर्जीवन के लिए
नदियाँ और तालाब केवल जलस्थल नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के आधार हैं। इन्हें पुनर्जीवित किए बिना चित्रकूट के भूगोल को बचाना संभव नहीं है।
तालाबों की खुदाई, गाद हटाना, नालों को पुनः जोड़ना और जल–संग्रहण की पारंपरिक प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाना जरूरी है।
5.3 खनन नियंत्रण के लिए
अनियंत्रित खनन पहाड़ों, वनों और जलस्रोतों को एक साथ नष्ट कर रहा है। खनन पर कठोर नियंत्रण और वैकल्पिक रोजगार–विकल्प के बिना
पर्यावरणीय संतुलन को बहाल नहीं किया जा सकता।
5.4 तापमान और जलवायु संतुलन के लिए
तापमान को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी रणनीति है—वन विस्तार, जलसंचयन और मिट्टी संरक्षण।
यदि गर्मी इसी तरह बढ़ती रही, तो चित्रकूट की धरती और अधिक बंजर और सूखी होती जाएगी।
5.5 कृषि और मिट्टी बचाने के लिए
मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाने का मतलब है कि आने वाले वर्षों में खेतों में बीज तो बोए जाएँगे, लेकिन उत्पादन धीरे-धीरे घटता जाएगा।
यह संकट सीधे किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा।
5.6 जैव-विविधता की रक्षा के लिए
वन्य जीवों के लिए जंगल और जलस्रोत जीवन का आधार हैं। जैसे-जैसे इनके आवास सिकुड़ते हैं, कई प्रजातियाँ या तो गायब हो जाएँगी या मानव बस्तियों की ओर
पलायन कर संघर्ष बढ़ाएँगी। जैव-विविधता का टूटना प्रकृति के पूरे संतुलन को बिगाड़ देगा।
5.7 धार्मिक–प्राकृतिक विरासत बचाने के लिए
चित्रकूट की आध्यात्मिक पहचान उसके प्राकृतिक स्वरूप पर टिकी हुई है। यदि पहाड़, जंगल, नदियाँ और गुफाएँ न रहें तो केवल इमारतें और बोर्ड ही बचेंगे,
जो उस जीवंत विरासत का स्थान कभी नहीं ले सकते, जिसकी जड़ें प्रकृति में धँसी हुई हैं।
6. संरक्षण के उपाय : वैज्ञानिक, व्यवहारिक और सामुदायिक रास्ता
6.1 खनन पर कठोर नियंत्रण
सबसे पहले तो संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में खनन को पूर्णतः प्रतिबंधित करना होगा। जहाँ खनन अनिवार्य रूप से जारी है, वहाँ पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन,
नियमित निगरानी और पुनर्वनीकरण (री–प्लांटेशन) अनिवार्य किया जाए।
6.2 वैज्ञानिक जल–संरक्षण
चेकडैम, परकोलेशन टैंक, पहाड़ी जल–कुंड, खेत–तालाब, और नालों को पुनर्जीवित करने जैसे उपायों से वर्षाजल को रोका और जमीन में उतारा जा सकता है।
इससे भूजल recharge होगा और तालाबों–कुओं में पानी अधिक समय तक टिक सकेगा।
6.3 वन पुनर्स्थापन
स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण, सामुदायिक वन–समितियाँ, ग्राम पंचायत स्तर पर “वन–संरक्षण संकल्प”,
और धार्मिक–स्थलों के आसपास “हरित–क्षेत्र” घोषित कर वन पुनर्स्थापन को गति दी जा सकती है।
6.4 पर्यटन प्रबंधन
मंदाकिनी और परिक्रमा मार्ग को प्लास्टिक–मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए, घाटों पर कचरा–डिब्बे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
सीवेज उपचार संयंत्र और सख्त जुर्माने की व्यवस्था बनाई जाए। धार्मिक यात्रियों के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाए कि “धर्म के नाम पर प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएँ”।
6.5 ग्रामीण जल–सुरक्षा मॉडल
प्रत्येक गाँव के लिए कम से कम दो तालाब, एक चेकडैम, और न्यूनतम 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा जाए।
पंचायत योजनाओं, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं को इससे जोड़ा जा सकता है, जिससे रोजगार के साथ–साथ जल–संरक्षण भी हो सके।
6.6 भूजल संरक्षण कानून
बोरवेल की अनियंत्रित खुदाई पर रोक के लिए स्थानीय स्तर पर भूजल–सुरक्षा कानून जरूरी है।
किस क्षेत्र में, कितनी गहराई तक, किस उद्देश्य के लिए बोरवेल की अनुमति दी जाए—इस पर स्पष्ट नियम बनें और उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई हो।
6.7 सामुदायिक भागीदारी
किसी भी पर्यावरणीय अभियान की सफलता स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर निर्भर होती है।
महिला स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब, स्कूल–कॉलेज, धार्मिक संस्थाएँ और ग्राम पंचायतें यदि जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लें,
तो सरकारी योजनाएँ भी जमीन पर अधिक प्रभावी रूप से उतर सकती हैं।
निष्कर्ष
चित्रकूट सचमुच खतरे में है—और यह खतरा अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की उपेक्षा, लालच, अनियोजित विकास और पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता का परिणाम है।
पहाड़, जंगल और नदियाँ सचमुच पुकार रही हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं।
यदि हमने अभी भी जल–संरक्षण, वन–संरक्षण, खनन–नियंत्रण और पर्यटन–प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए,
तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल पुस्तकों और कहानियों में ही उस चित्रकूट को खोजेंगी, जो कभी प्रकृति और अध्यात्म के अद्भुत संगम के रूप में जाना जाता था।
समय की माँग है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन, वैज्ञानिक, सामाजिक संगठन और आम लोग मिलकर चित्रकूट के भूगोल और पर्यावरण को बचाने की एक संयुक्त मुहिम शुरू करें।
क्योंकि चित्रकूट को बचाना केवल एक जिले को बचाना नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की आत्मा, उसकी मिट्टी, उसके जंगल, उसकी नदियों और उसकी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है।