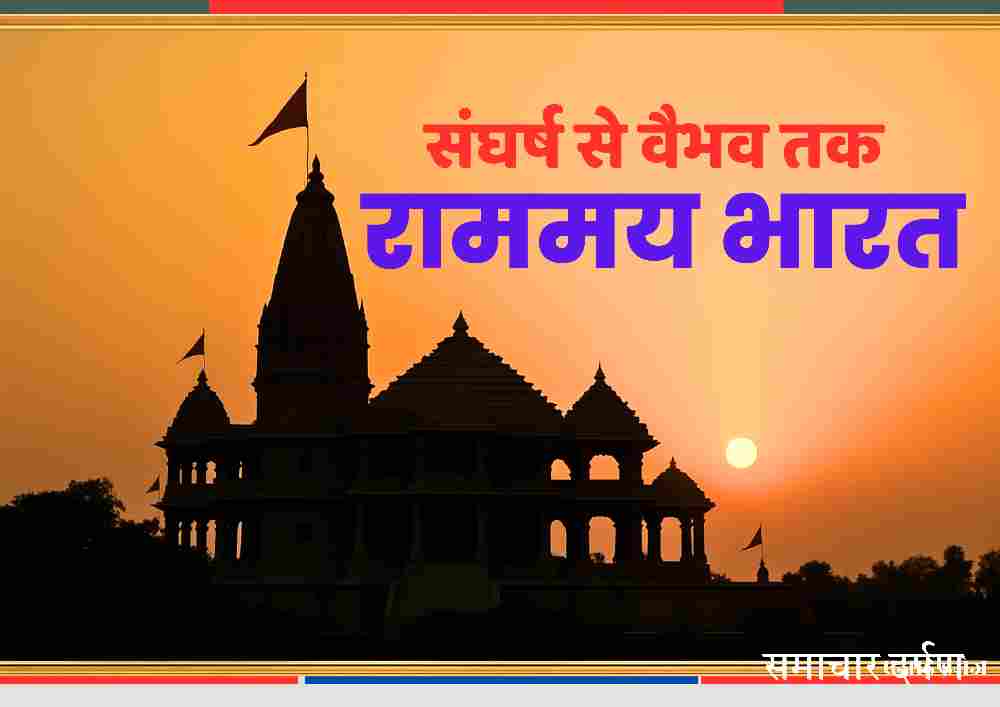
अयोध्या में भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के शिखर पर धर्म–ध्वजा फहराने के साथ ही सदियों का संघर्ष और प्रतीक्षा पूर्णता की ओर बढ़ा। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ धार्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का एक अनोखा क्षण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भारत अब राममय है” वाले कथन ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धाभाव को नई ऊंचाई दे दी। हालांकि, एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश के गंभीर विश्लेषण में यह सवाल भी उभरता है कि क्या वास्तव में भारत सिर्फ “राममय” है या फिर “सर्वमय”?
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अयोध्या का कायाकल्प असाधारण है। पर्यटन, अवसंरचना, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आकर्षण के कारण यह शहर आर्थिक रूप से अत्यधिक विकसित हो चुका है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पंचतारा होटल, चौड़ी सड़कें और विशाल पर्यटन ढांचा अयोध्या को वैश्विक धार्मिक राजधानी के रूप में स्थापित कर चुके हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक अयोध्या की पर्यटन अर्थव्यवस्था 18,000 करोड़ रुपए पार करेगी और शहर का जीडीपी पहले ही 10,000 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। करोड़ों भक्तों की आमद ने स्थानीय व्यवसायों, रोजगार और उद्योग को नई गति दी है। परंतु यह सवाल भी दिमाग में रहता है कि धर्म–आधारित अर्थव्यवस्था सामाजिक असंतुलन का कारण तो नहीं बनेगी?
राम भारतीय चेतना के शिखर पुरुष हैं। उनका आदर्श, त्याग, करुणा, न्याय और मर्यादा आज भी जीवन मूल्यों का आधार है। संदेह नहीं कि भारतीय सभ्यता राम के बिना अधूरी है। लेकिन भारतीय पहचान राम पर ही समाप्त हो जाती है—यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं।
भारत शिवमय भी है, कृष्णमय भी, देविमय भी, जैनमय भी, बौद्धमय भी। भारत सिख गुरुओं के बलिदान से भरा है, और ईसाई व इस्लामिक आस्थाओं से भी प्रभावित है। भारत का सार बहुलता है, एकांगीपन नहीं।
यदि सनातन की रक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई की बात हो तो इतिहास केवल अयोध्या तक सीमित नहीं।
छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर — सभी ने धर्म, देश और अस्मिता की रक्षा के लिए महान बलिदान दिए।
यदि राम राष्ट्र के गौरव का प्रतीक हैं तो ये सभी पुरोधा भी राष्ट्र की सांस्कृतिक रीढ़ हैं। इसलिए यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि अयोध्या मंच पर “राममय भारत” का नारा तो दिया गया, लेकिन “गुरुमय”, “शिवमय” या “भारत सर्वमय” के लिए वैसा ही भाव क्यों नहीं?
भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता हैं, किसी एक धर्म के नहीं।
भले ही बहुत कम मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन इससे यह सत्य नहीं बदल जाता कि वे भी इस राष्ट्र के समान अधिकार संपन्न नागरिक हैं।
राजनीतिक मंच से धार्मिक भाषा का अत्यधिक उपयोग कभी–कभी असंतुलन की इबारतें लिख सकता है।
भारत तभी विश्वगुरु बनेगा जब यहां हर धर्म, हर आस्था और हर सांस्कृतिक इकाई को समान सम्मान मिलेगा।
अयोध्या मॉडल सफल है, लेकिन यह अंतिम मॉडल नहीं हो सकता।
यह आवश्यक है कि काशी, मथुरा, अमृतसर, बोधगया, पुष्कर, अजमेर और उज्जैन जैसे तीर्थ भी समान निवेश और संवेदना प्राप्त करें।
सांस्कृतिक गर्व तभी स्थायी होगा जब वह संतुलित, समावेशी और न्यायपूर्ण होगा।
क्या राम मंदिर की स्थापना भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है?
लेकिन यह पुनर्जागरण तभी संतुलित और सार्थक माना जाएगा, जब भारत को केवल ‘राममय’ नहीं,
बल्कि ‘सर्वमय’ — यानी हर धर्म, हर आस्था और हर सांस्कृतिक परंपरा का संगम — समझा जाए।
क्या अयोध्या का विकास मॉडल अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक शहरों पर भी लागू किया जा सकता है?
को भी बेहतर अवसंरचना, स्वच्छता, सुरक्षा और रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जा सकता है।
लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि विकास का आधार केवल धार्मिक भावनाएँ न होकर
व्यापक सार्वजनिक हित, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समाज की ज़रूरतें भी हों।
क्या “राममय भारत” की राजनीतिक भाषा भारतीय बहुलता को सीमित करती है?
तो अन्य आस्थाएँ स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकती हैं।
इसलिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक दृष्टि से “भारत सर्वमय है” जैसा भाव
ज़्यादा संतुलित और समावेशी माना जाएगा, क्योंकि इसमें राम के साथ–साथ
शिव, कृष्ण, बुद्ध, नानक, ईसा और अल्लाह में आस्था रखने वाले सभी नागरिकों के लिए जगह है।
क्या धर्म–आधारित पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में सुरक्षित मानी जा सकती है?
लेकिन दीर्घकाल में केवल इसी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।
एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को उद्योग, कृषि, शिक्षा, तकनीक और सेवाक्षेत्र जैसे विविध आधारों पर खड़ा होना चाहिए।
धार्मिक पर्यटन इन सबका पूरक बने, आधार नहीं — यही अधिक सुरक्षित और विवेकपूर्ण मॉडल होगा।
