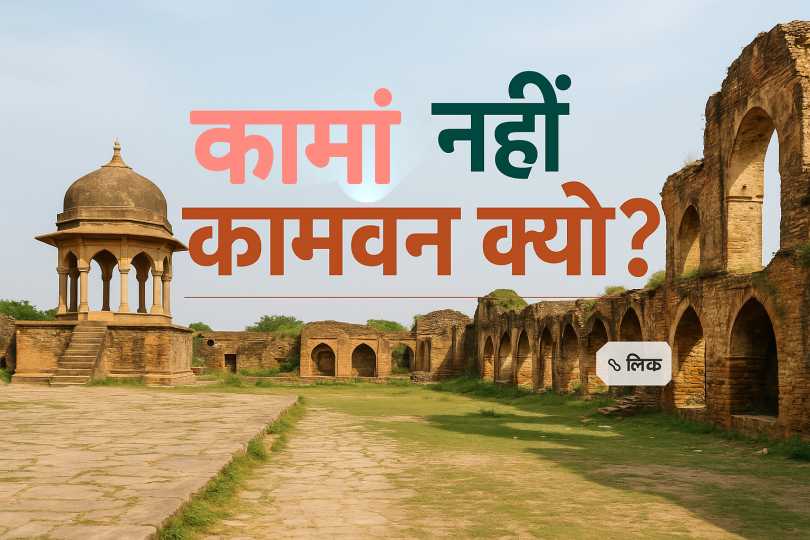
हिमांशु मोदी की रिपोर्ट
राजस्थान के भरतपुर जिले के पास स्थित कस्बा कामां, पिछले कुछ समय से एक नए विवाद की वजह से सुर्खियों में है।
स्थानीय संत समाज, ब्रज संस्कृति से जुड़े संगठन और कुछ जनप्रतिनिधि इस कस्बे का नाम बदलकर
“कामवन” या “बृज नगरी कामवन” करने की मांग लगातार उठा रहे हैं।
उनका कहना है कि यह क्षेत्र प्राचीन ब्रज वन “काम्यवन/कामवन” की धरती है, जबकि “कामां” शब्द केवल उसका अपभ्रंश और ऐतिहासिक विकृति है।
सवाल यह है कि – “कामां नहीं कामवन क्यों?” और यह मांग तर्क के कसौटी पर कितनी सुसंगत दिखती है?
यह विश्लेषणात्मक फीचर न केवल नाम बदलने की मांग के पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक तर्कों पर रोशनी डालता है,
बल्कि इतिहास, भाषा, स्थानीय समाज, प्रशासनिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक विमर्श के संदर्भ में भी इस मुद्दे को परखने की कोशिश करता है।
साथ ही, यह लेख कामां–कामवन विवाद को व्यापक रूप से चल रही “नाम बदलने की राजनीति” के संदर्भ में भी देखने का प्रयास करता है।
ब्रज की देहरी पर बसा कस्बा: कामां की भौगोलिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
कामां राजस्थान के पूर्वी हिस्से में स्थित वह कस्बा है, जिसे एक ओर प्रशासनिक रूप से भरतपुर–डीग क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है,
तो दूसरी ओर सांस्कृतिक दृष्टि से यह खुद को ब्रज मंडल से जोड़कर देखता है।
स्थानीय परंपरा में कामां को “आदि वृंदावन” कहने की परिपाटी भी मिलती है।
कहा जाता है कि यहाँ कभी कदंब और तुलसी के घने वन थे, जिनमें श्रीकृष्ण की अनेक लीलाओं की स्मृति लोककथाओं में सहेजी जाती है।
ब्रज परिक्रमा मार्ग पर यह क्षेत्र महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
संत-महात्मा और भक्त वर्ग कामां को “चौरासी तीर्थों की भूमि” के रूप में भी वर्णित करते हैं,
जहाँ 84 कुण्डों, 84 मंदिरों और अनेक प्राचीन स्थलों का उल्लेख मिलता है।
इसी धार्मिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने आगे चलकर कामां को कामवन से जोड़ने की मांग को बल दिया।
काम्यवन से कामवन और फिर कामां तक: नामों का इतिहास और परंपरा
ब्रज साहित्य और वैष्णव परंपरा में ब्रज के द्वादश वन – जैसे मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन आदि – का उल्लेख मिलता है।
इन्हीं में से एक वन काम्यवन या कामवन है, जहाँ श्रीकृष्ण की रासलीला, गोचारण और गोपियों के साथ अनेक लीलाओं की कथाएँ सुनाई जाती हैं।
माना जाता है कि कामां का भू–भाग इसी काम्यवन की परिधि में आता था और समय के साथ बोलचाल में काम्यवन → कामवन → कामन/कामां जैसा रूपांतरण हुआ।
आधुनिक प्रशासनिक रिकॉर्ड में यह कस्बा अंग्रेज़ी में “Kaman” के रूप में दर्ज हो गया, जिसे हिंदी बोलचाल में “कामां” कहा जाने लगा।
कई स्थानीय मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि किसी समय यह क्षेत्र “ब्राह्मपुर” या किसी अन्य नाम से भी जाना गया होगा,
लेकिन वर्तमान पीढ़ियाँ इसे मुख्य रूप से कामां के नाम से ही पहचानती हैं।
नामों की यह बहुलता बताती है कि इतिहास कभी एकरेखीय नहीं होता।
एक ही भू–भाग पर अलग–अलग काल में भिन्न–भिन्न नाम और कथाएँ परतों की तरह चढ़ती चली जाती हैं।
आज की बहस इसी बात पर केंद्रित है कि –
इन परतों में से किसको “मूल” माना जाए, और किसे “अपभ्रंश” या “विकृति” घोषित कर दिया जाए।
कामां का नाम बदलकर “कामवन” करने की मांग कहाँ से और कैसे उठी?
पिछले कुछ वर्षों में ब्रज क्षेत्र की धार्मिक यात्राओं और कथावाचन परंपराओं में
कामां को “कामवन” के रूप में प्रचारित किए जाने की प्रवृत्ति तेज़ हुई है।
संत समाज और कुछ संगठनों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में यह बात जोर–शोर से उठानी शुरू की कि
“यह भूमि प्राचीन कामवन की है, इसे बृज नगरी कामवन के नाम से जाना जाना चाहिए।”
इसके बाद स्थानीय स्तर पर ज्ञापन, धरना और धार्मिक सभाएँ आयोजित हुईं, जिनमें प्रशासन से यह मांग की गई कि
सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज “कामां/Kaman” की जगह आधिकारिक रूप से “कामवन” नाम लिखे जाएँ।
इसी बीच क्षेत्र के विधायक द्वारा भी मीडिया और मंचों पर इस मांग का समर्थन किया गया और
कहा गया कि वे इसे विधानसभा और सरकार के समक्ष उठाएँगी।
इसके बाद कामां–कामवन विवाद केवल धार्मिक आग्रह नहीं रहा, बल्कि औपचारिक राजनीतिक मुद्दा बन गया।
समर्थकों के तर्क: “कामवन” नाम के पक्ष में क्या-क्या कहा जा रहा है?
. “शास्त्र–सम्मत नाम” और ब्रज–परंपरा का तर्क
नाम बदलने के पक्ष में सबसे प्रमुख तर्क यह दिया जा रहा है कि
“कामवन/काम्यवन नाम शास्त्र और पुरानी ब्रज–परंपरा में मिलता है, जबकि ‘कामां’ केवल उसका अपभ्रंश है।”
समर्थकों का कहना है कि ब्रज मंडल परिक्रमा, पुरानी वंशावली कथाओं और वैष्णव ग्रंथों में जिस स्थान का उल्लेख मिलता है,
वह “कामवन” है, न कि कामां।
इसलिए “कामां” को “त्रुटि” मानकर इसे “ठीक” करना धार्मिक और ऐतिहासिक न्याय की दिशा में कदम होगा।
ब्रज–पर्यटन, ब्रांडिंग और आस्था–आधारित अर्थव्यवस्था
दूसरा बड़ा तर्क पर्यटन और आस्था–आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा है।
वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगाँव जैसे स्थलों ने अपने धार्मिक नामों के कारण ही वैश्विक पहचान पाई है।
समर्थकों का मानना है कि यदि कामां को “बृज नगरी कामवन” के रूप में आधिकारिक मान्यता मिलती है,
तो यह सीधे–सीधे ब्रज के 12 वनों की श्रृंखला से जुड़ जाएगा और देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
बढ़ता हुआ धार्मिक पर्यटन स्थानीय स्तर पर होटल, धर्मशाला, परिवहन, प्रसाद–व्यापार, हस्तशिल्प और छोटे–मोटे कारोबारों को मजबूती दे सकता है।
इस दृष्टि से नाम परिवर्तन को एक तरह से “आस्था + अर्थव्यवस्था” मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है।
“काम” शब्द की नकारात्मक ध्वनि से दूरी और “वन” की पवित्रता
कुछ धार्मिक नेताओं और स्थानीय नागरिकों का मानना है कि “कामां” शब्द आम बोलचाल में “काम” (वासना/इच्छा) की ओर संकेत करता है,
जबकि “कामवन” में “वन” की पवित्र, तपस्या और भक्ति–केंद्रित छवि उभरती है।
उनके अनुसार “कामवन” नाम सुनते ही मन में रासलीला, भक्ति, तप, त्याग और श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ी भावनाएँ जागती हैं,
जबकि “कामां” शब्द वही आध्यात्मिक गूंज नहीं पैदा कर पाता।
इस दृष्टि से यह मांग केवल इतिहास या परंपरा नहीं, बल्कि “ध्वन्यार्थीय शुद्धिकरण” यानी
शब्द की ध्वनि और अर्थ को शुद्ध व पवित्र बनाने के प्रयास के रूप में भी देखी जा सकती है।
विरोध और सवाल: क्या केवल नाम बदलने से सब ठीक हो जाएगा?
जहाँ एक ओर समर्थक “कामवन” नाम को धार्मिक–सांस्कृतिक न्याय बताते हैं,
वहीं दूसरी ओर कई लोग इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाते हैं।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल नाम बदल देने से क्षेत्र की वास्तविक समस्याएँ हल हो जाएँगी?
बहु–सांस्कृतिक समाज और मेवात की संवेदनशीलता
कामां केवल ब्रज–हिंदू पहचान वाला इलाका ही नहीं, बल्कि मेवात की सीमा से लगा बहु–सांस्कृतिक क्षेत्र भी है,
जहाँ मेव मुस्लिम समुदाय सहित अनेक सामाजिक–धार्मिक समूह निवास करते हैं।
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक चिंता उठती है कि क्या नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में सभी समुदायों की राय को समान महत्व दिया जाएगा या नहीं।
अगर नाम बदलने का निर्णय केवल एक धार्मिक दृष्टि या एक वर्ग की मांग पर आधारित दिखे,
तो इससे समाज में यह संदेश जा सकता है कि नगर की पहचान केवल एक ही सांस्कृतिक धुरी से तय होगी।
इससे समावेशी पहचान के बजाय एकांगी पहचान को बढ़ावा मिलने का खतरा भी आलोचक व्यक्त करते हैं।
इतिहास और भाषा की बहुलता बनाम “एकमात्र शुद्ध नाम” की धारणा
ऐतिहासिक रूप से किसी भी कस्बे या नगर के कई नाम रहे होते हैं।
समय के साथ राजसत्ता, धर्म, भाषा और समाज–व्यवस्था के बदलने पर नाम भी बदलते हैं।
ऐसे में यह कहना कि “कामवन ही असली नाम है और कामां केवल गलती”,
इतिहास की बहुलता को नज़रअंदाज़ करने जैसा भी हो सकता है।
भाषा–विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शब्दों का अपभ्रंश होना और उनका नया रूप ही “मानक” बन जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है।
हो सकता है कि कामवन से कामां बना हो, लेकिन सदियों से जीवित और प्रचलित नाम को केवल “त्रुटि” कहकर खारिज कर देना,
कई विद्वानों के लिए स्वीकार्य नहीं है।
अधिक संतुलित दृष्टिकोण यह कहता है कि – “कामवन धार्मिक–परंपरागत नाम है और कामां लोकभाषा व प्रशासन का नाम; अब प्रश्न यह है कि किसे प्राथमिकता दी जाए।”
प्रशासनिक बोझ और स्थानीय विकास के मूल मुद्दे
किसी भी शहर या कस्बे का नाम बदलने से केवल बोर्ड या पट्टिकाएँ नहीं बदलतीं,
बल्कि सरकारी फाइलें, भूमि अभिलेख, विद्यालय प्रमाणपत्र, बैंक रिकॉर्ड, पहचान पत्र, वाहन पंजीयन आदि लगभग हर जगह सुधार करना पड़ता है।
यह पूरा काम समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की भारी मांग करता है।
आलोचक सवाल उठाते हैं कि जब क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, अस्पताल, बेरोज़गारी, सड़क और भ्रष्टाचार जैसे ठोस मुद्दे मौजूद हों,
तो क्या प्राथमिकता नाम बदलने को दी जानी चाहिए या इन मूलभूत समस्याओं के समाधान को?
कई नागरिकों के लिए यह चिंता भी महत्वपूर्ण है कि कहीं “नाम की राजनीति” के चलते विकास के वास्तविक मुद्दे पीछे न छूट जाएँ।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सबकी सहमति का सवाल
किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील निर्णय की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि
उसमें जनभागीदारी और पारदर्शिता कितनी है।
यदि ग्राम सभाओं, नगर निकायों, सभी समुदायों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के साथ व्यापक संवाद के बाद सहमति बने,
तो निर्णय को अधिक वैधता मिलती है।
लेकिन यदि पूरी प्रक्रिया केवल ऊपर–ऊपर से चले, कुछ ज्ञापनों और मंचीय घोषणाओं पर आधारित रहे,
और आम जनता को लगा कि उनकी राय पूछे बिना ही फैसला थोप दिया गया है,
तो तर्क की सुसंगति पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।
इसलिए प्रक्रिया की लोकतांत्रिक मजबूती इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी बन जाती है।
तर्क की सुसंगति: तीन स्तरों पर संक्षिप्त मूल्यांकन
कामां का नाम बदलकर कामवन करने की मांग को अगर तीन अलग–अलग स्तरों पर परखा जाए,
तो तस्वीर कुछ इस प्रकार सामने आती है –
1. धार्मिक–सांस्कृतिक स्तर पर:
ब्रज परंपरा, काम्यवन का उल्लेख, 84 तीर्थों की मान्यता और ब्रज–परिक्रमा की धारणा को देखें,
तो “कामवन” नाम धार्मिक–भावनात्मक दृष्टि से काफी सशक्त और सुसंगत दिखता है।
यह नाम ब्रज की पहचान को मजबूत करता है और आस्था के साथ सहज रूप से जुड़ता है।
2. ऐतिहासिक–भाषाई स्तर पर:
यहाँ तर्क उतना एकरेखीय नहीं है।
कामवन को प्राचीन और कामां को अपभ्रंश मानना आंशिक रूप से संभव है,
लेकिन इतिहास और भाषा की स्वाभाविक प्रक्रियाओं को देखते हुए “कामां को पूरी तरह गलत” घोषित करना अतिरंजना भी हो सकता है।
अधिक संतुलित नजरिया यह मानता है कि दोनों नाम अलग–अलग काल और संदर्भ के प्रतिनिधि हैं।
3. लोकतांत्रिक–सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर:
यहाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया कितनी समावेशी, पारदर्शी और न्यायपूर्ण है।
अगर सभी समुदायों की राय लेकर, खुले विमर्श और कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला हो,
तो इसे “लोकतांत्रिक निर्णय” कहा जा सकता है;
अन्यथा नाम परिवर्तन को “सांकेतिक राजनीति” समझने वालों की संख्या कम नहीं होगी।
कामां बनाम कामवन – असली सवाल नाम का नहीं, अर्थ और भागीदारी का है
अंततः सवाल केवल इतना नहीं है कि इस कस्बे का आधिकारिक नाम कामां रहे या कामवन बन जाए।
असली सवाल यह है कि – इस भूमि की पहचान कैसी हो, इतिहास की कौन–सी परत को “अंतिम सत्य” माना जाए,
ब्रज–परंपरा को कितना और किस रूप में महत्व दिया जाए,
और इस पूरे निर्णय में स्थानीय समाज की भागीदारी कितनी व्यापक हो।
जो लोग “कामवन” नाम के पक्ष में हैं, उनके लिए यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि
ब्रज की आध्यात्मिक स्मृतियों, आस्था, पर्यटन और गौरव–बोध का प्रतीक है।
वहीं, जो लोग इस परिवर्तन पर सवाल उठाते हैं,
वे इतिहास की बहुलता, समाज की विविधता और विकास के ठोस मुद्दों को नज़रअंदाज़ न करने की बात करते हैं।
लोकतंत्र में किसी भी नाम का असली अर्थ तभी सार्थक होता है,
जब उसमें स्थानीय लोगों की सहमति, सम्मान और साझेदारी शामिल हो।
कामां हो या कामवन, यदि इस बहस के रास्ते समाज संवाद करना सीखता है,
एक–दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और अपने क्षेत्र के वास्तविक मुद्दों पर मिल–बैठकर विचार करता है,
तभी यह विवाद किसी सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुँच सकेगा।
क्लिक करें और पढ़ें: सवाल–जवाब
प्रश्न 1: कामां का नाम कामवन रखने की मांग क्यों की जा रही है?
समर्थकों का मानना है कि कामां क्षेत्र प्राचीन ब्रज वन “काम्यवन/कामवन” की धरती है।
उनके अनुसार “कामां” शब्द “कामवन” का अपभ्रंश है,
जबकि शास्त्र और परंपरा में इस क्षेत्र का उल्लेख कामवन के नाम से मिलता है।
इसलिए वे चाहते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में भी इस कस्बे को “कामवन” या “बृज नगरी कामवन” के नाम से दर्ज किया जाए।
प्रश्न 2: क्या कामां भरतपुर का हिस्सा है या ब्रज का?
प्रशासनिक रूप से कामां राजस्थान के भरतपुर–डीग क्षेत्र का हिस्सा है।
लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में इसे ब्रज मंडल का अंग माना जाता है।
यही कारण है कि यहाँ ब्रज से जुड़ी कथाएँ, परिक्रमा परंपरा और श्रीकृष्ण–लीला से संबंधों पर ज़ोर दिया जाता है।
प्रश्न 3: कामां से कामवन नाम बदलने से क्या फायदे बताए जा रहे हैं?
समर्थकों के अनुसार नाम बदलने के तीन प्रमुख फायदे होंगे –
(1) ब्रज परंपरा के अनुरूप “कामवन” नाम से धार्मिक–सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी,
(2) ब्रज–पर्यटन और तीर्थ–यात्रा में इस कस्बे की स्थिति और प्रमुख हो सकती है,
(3) स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, प्रसाद–व्यापार और अन्य छोटे कारोबारों को आर्थिक लाभ मिल सकता है।
प्रश्न 4: क्या सभी समुदाय इस नाम परिवर्तन की मांग से सहमत हैं?
इस विषय पर समाज के भीतर मतभेद मौजूद हैं।
कुछ लोग धार्मिक और सांस्कृतिक तर्कों के आधार पर “कामवन” नाम को सही मानते हैं,
जबकि अन्य लोग इतिहास की बहुलता, मेवात की सांस्कृतिक विविधता,
प्रशासनिक बोझ और विकास के वास्तविक मुद्दों की अनदेखी की चिंता जताते हैं।
इसलिए यह कहना मुश्किल है कि पूरी आबादी एक मत से नाम परिवर्तन के पक्ष में है;
यहाँ व्यापक संवाद और वास्तविक जनमत की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
“`0







